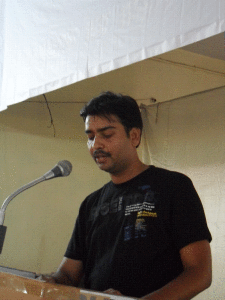भारत का मजदूर आन्दोलन और कम्युनिस्ट आन्दोलन : अतीत के सबक, वर्तमान समय की सम्भावनाएँ तथा चुनौतियाँ
द्वितीय अरविन्द स्मृति संगोष्ठी में प्रस्तुत आलेख
सुखविन्दर
सम्पादक, ‘प्रतिबद्ध’, लुधियाना
”इतिहास अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में मनुष्य की गतिविधि के सिवा कुछ नहीं है।”
– कार्ल मार्क्स, पवित्र परिवार
द्वितीय अरविन्द स्मृति संगोष्ठी में उपस्थित साथियो,
जब मनुष्य अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रयत्न करता है तो इस प्रक्रिया में अतीत के प्रयोगों की शिक्षा की रोशनी में आगे बढ़ते हुए कई भूलें करता है, कभी सफल होता है तो कभी असफल। और अपने इन प्रयासों की नकारात्मक तथा सकारात्मक शिक्षाएँ आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है।
भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन का इतिहास लगभग नब्बे साल पुराना है। भारतीय मजदूर वर्ग इसके करीब चार दशक पहले से ही पूँजीवादी शोषण के विरुध्द संगठित संघर्षों की शुरुआत कर चुका था। मजदूर वर्ग के संघर्षों के जुझारूपन और कम्युनिस्टों की कुर्बानी, वीरता और त्याग पर शायद ही कोई सवाल उठा सकता है। लेकिन व्यापक सर्वहारा आबादी को नये सिरे से आर्थिक-राजनीतिक संघर्षों के लिए संगठित करने तथा उनके बीच मजदूर क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन का प्रचार करने की समस्याओं से जूझते हुए जब हम इतिहास का पुनरावलोकन करते हैं तो मजदूर आन्दोलन में कम्युनिस्ट पार्टी के काम को लेकर बहुत सारे प्रश्नचिह्न उठ खड़े होते हें।
यह लेनिनवाद की बुनियादी सर्वमान्य प्रस्थापना है कि उजरती ग़ुलामी के विरुध्द स्वत: उठ खड़ा होने वाला मजदूर आन्दोलन अपने आप, अपनी स्वतन्त्र गति से, समाजवाद के लिए संघर्ष नहीं बन जाता। इस सोच को लेनिन ने अर्थवादी, स्वत:स्फूर्ततावादी और संघाधिपत्यवादी सोच बताया था। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि (1) आर्थिक संघर्ष स्वयंस्फूर्त गति से राजनीतिक संघर्ष नहीं बना जाता, (2) कम्युनिस्टों को आर्थिक संघर्ष के साथ-साथ राजनीतिक माँगों के संघर्ष को आगे बढ़ाना और उन्नततर धरातल पर ले जाना होता है तथा साथ-साथ मजदूर वर्ग के बीच राजनीतिक शिक्षा एवं प्रचार की कार्रवाई चलानी होती है (यानी मजदूर आन्दोलन में वैज्ञानिक समाजवाद का विचार स्वत: नहीं पैदा हो जाता, बल्कि बाहर से डालना पड़ता है, (3) वर्ग संघर्ष की प्राथमिक पाठशाला के रूप में ट्रेड यूनियनों का महत्व अनिवार्य है, लेकिन एक राजनीतिक अखबार व अन्य माध्यमों से उन्नत चेतना वाले मजदूर तत्वों को मार्क्सवादी विचारधारा तक लाना और पार्टी-निर्माण को अंजाम देना सर्वहारा क्रान्ति की दिशा में आगे बढ़ने की बुनियादी शर्त है।
इन बुनियादी लेनिनवादी कसौटियों पर जब हम भरत के मजदूर आन्दोलन में कम्युनिस्ट पार्टी के काम को देखते हैं तो 1920 से लेकर 1951 तक लगातार हमें ऐसी गम्भीर कमियाँ नजर आती हैं जिन्हें अर्थवादी ट्रेड यूनियनवादी भटकाव कहा जा सकता है। हम 1951 के बाद की कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि तब वह पूर्णत: संशोधनवादी पार्टी बन चुकी थी। आगे इतिहास के पर्यवेक्षण के दौरान हम देखेंगे कि विचारधारात्मक दृष्टि से कमजोर और ढीले-ढाले बोल्शेविक ढाँचे वाली भारत की कम्युस्टि पार्टी ने मजदूरों का जबरदस्त समर्थन हासिल होने के बावजूद उनके बीच व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक काम कभी नहीं किया। आश्चर्य नहीं कि ऐसे में राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व सर्वहारा वर्ग के हाथों में नहीं आ पाया और मुक्तिकामी जनसमुदाय के बीच सर्वहारा राजनीति का वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाया। 1951 से 1967 तक संशोधनवादी भाकपा-माकपा से यह अपेक्षा की नहीं जा सकती थी। फिर नक्सलबाड़ी उभार से जो नयी लहर पैदा हुई वह ”वामपन्थी” आतंकवाद के भँवर में जा फँसी। मजदूर वर्ग के बीच पार्टी कार्य व जनकार्य की समस्याओं पर सोचना उसका एजेण्डा बना ही नहीं। इसमें से जो लोग जनदिशा की बात करते हुए अलग धाराओं-उपधाराओं में संगठित हुए, वे भी जनवादी क्रान्ति की गलत समझ के साथ ज्यादातर मालिक किसानों के लागत मूल्य-लाभकारी मूल्य की लड़ाई में उलझकर रह गये और मजदूरों में कहीं कुछ काम भी किया तो वह जुझारू अर्थवाद से अधिक कुछ भी नहीं था। आज जब हम भूमण्डलीकरण की नयी परिस्थितियों में मजदूर वर्ग को नये सिरे से संगठित करने की चुनौतियों पर सोच रहे हैं तो भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन और मजदूर आन्दोलन के सम्बन्ध पर – मजदूरों के बीच आर्थिक कार्य और राजनीतिक कार्य के सम्बन्ध के व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचना-विचारना बेहद जरूरी है। इसी सन्दर्भ में हमने इतिहास पर एक संक्षिप्त पश्चदृष्टि डालने की और जरूरी नतीजे निकालने की एक कोशिश की है।
एक संक्षिप्त ऐतिहासिक सिंहावलोकन और कुछ जरूरी नतीजे
भारत में मजदूर आन्दोलन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। औपनिवेशिक भारत में हुए पूँजीवादी विकास के चलते भारतीय इतिहास के रंगमंच पर दो नये वर्गों का उदय हुआ। एक ओर जहाँ औद्योगिक पूँजीपति वर्ग का जन्म हुआ वहीं दूसरी तरफ मानव इतिहास का सर्वाधिक क्रान्तिकारी वर्ग औद्योगिक मजदूर वर्ग अस्तित्व में आया। यह वर्ग अतीत के शोषित-उत्पीड़ित क्रान्तिकारी वर्गों – ग़ुलामों तथा किसानों से भिन्न है। यह वर्ग ग़ुलामों तथा किसानों की तरह हजारों साल वर्गीय शोषण-उत्पीड़न झेलने को तैयार नहीं है। यह अस्तित्व में आते ही पूँजीपति वर्ग के खिलाफ युध्द में जुट जाता है। भारत में कई उतार-चढ़ावों से गुजरते, कभी थोड़ी देर के ठहराव के बाद फिर तूफानी गति से आगे बढ़ते मजदूर आन्दोलन का एक अविराम सिलसिला जारी रहा है जो हमेशा पहले औपनिवेशिक तथा 1947 के बाद देशी हुक्मरानों की नींद हराम करता रहा है।
19वीं सदी के मध्य में भारत में आधुनिक उद्योग (नील, चाय, कॉफी आदि) स्थापित हुए। 1850 से, 55 कोयला खदानों की शुरुआत हुई। 1879 में यहाँ 56 सूती मिलें और 1882 में 20 जूट मिलें थीं। 1880 से 1895 के बीच यहाँ 144 सूती मिलें और 29 जूट मिलें और 123 कोयला खदानें थीं। 1913-14 में भारत में सूती मिलों की संख्या बढ़कर 274 तथा जूट मिलों की संख्या 64 हो गयी। कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या उस समय 1,51,273 थी। 1940 में भारत में एक हजार कारखाने थे जिनमें 17 लाख मजदूर काम करते थे। कारखाने चाहे अंग्रेजों के हों या भारतीय पूँजीपतियों के, मजदूर भयंकर गरीबी तथा शोषण-उत्पीड़न के शिकार थे। उन्हें नारकीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता था (आज भी मजदूरों के हालात ऐसे ही हैं) और इन नारकीय परिस्थितियों के खिलाफ मजदूर जल्द ही संघर्ष के मैदान में उतर आये। जैसे-जैसे मजदूरों की ताकत बढ़ती गई, मजदूरों के संघर्ष अधिकाधिक उग्र, व्यापक, संगठित तथा योजनाबध्द भी होते गये। भले ही औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मजदूरों की संख्या बहुत कम थी, मगर, मुम्बई, कोलकाता, अहमदाबाद, कानपुर, शोलापुर तथा अन्य बड़े शहरों में उनके संकेद्रण ने उनकी मारक क्षमता को बढ़ाया।
औपनिवेशिक भारत का इतिहास अनेक बड़े मजदूर उभारों का साक्षी रहा है। 19वीं शताब्दी के आठवें दशक से ही स्वत:स्फूर्त मजदूर आन्दोलनों का सिलसिला जोर पकड़ने लगा था। 1882 से 1890 के बीच बाम्बे तथा मद्रास में 25 महत्वपूर्ण हड़तालें हुईं, तथा 1892-93 और 1901 के बीच बाम्बे में कई बड़ी हड़तालें हुईं। (सुमित सरकार, माडर्न इण्डिया½
1905 से 1908 के बीच स्वदेशी तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आन्दोलनों के प्रत्यक्ष प्रभाव से मजदूर आन्दोलन में एक उभार आया। 1908 में भारत के मजदूर आन्दोलन के इतिहास की एक अहम घटना घटी। 1908 में राष्ट्रवादी नेता तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में राजनीतिक हड़तालें करके बम्बई की सूती मिलों के मजदूरों ने अपनी प्रथम राजनीतिक कार्रवाई की थी और राजनीतिक चेतना एवं परिपक्वता का परिचय दिया था। जब 24 जून 1908 को बम्बई में तिलक की गिरफ्तारी हुई, तो न सिर्फ बम्बई में, बल्कि शोलापुर, नागपुर इत्यादि स्थानों पर तुरन्त विरोध का एक तूफान उमड़ पड़ा। तिलक के खिलाफ मुकदमा चलने के दौरान बम्बई के मजदूरों ने विशाल प्रदर्शन और हड़तालें कीं, जिनमें अकसर पुलिस और सेना से झड़पें हो जाती थीं। 18 जुलाई को सड़कों पर हुई एक ऐसी लड़ाई में कई हजार मजदूर घायल हुए और कई मारे गए। अगले दिन करीब 60 मिलों के 65 हजार मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 21 जुलाई को गोदी मजदूर भी हड़ताल में शामिल हो गए। 22 जुलाई को तिलक को 6 वर्ष की बामशक्कत कैद की सजा सुनायी गयी और हड़ताली मजदूरों ने 6 दिनों तक बम्बई को युध्द क्षेत्र में बदल दिया। इस संघर्ष का हवाला देते हुए लेनिन ने 5 अगस्त 1908 को कहा था, ”एक जनवादी व्यक्ति (अर्थात तिलक) के खिलाफ पूँजीपतियों के पालतू कुत्तों द्वारा की गयी इस प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के फलस्वरूप बम्बई में सड़कों पर प्रदर्शन और हड़ताल भड़क उठी है। भारत में भी सर्वहारा अब सचेत राजनीतिक जनसंघर्ष के स्तर तक विकसित हो चुका है (कलेक्टेड वर्क्स, खण्ड 15, पृष्ठ 184)। इसके अलावा इसी समय बंगाल, मद्रास, पंजाब आदि में मजदूरों के अनेकों छोटे-बड़े संघर्ष हुए।
इस समय तक का मजदूर आन्दोलन का इतिहास दर्शाता है कि मजदूर वर्ग ने सिर्फ अपने आर्थिक हितों के लिए ही संघर्ष नहीं लड़ा, बल्कि समग्र रूप से भारतीय जनता के सामान्य राजनीतिक हितों के लिए अधिक वीरतापूर्ण संघर्ष चलाया। मगर इस समय तक या तो मजदूर आन्दोलन स्वयं:स्फूर्त ढंग से हुए या उन पर राष्ट्रवादियों का प्रभाव रहा। मगर 1908 की गर्मियों के बाद मजदूर आन्दोलन में राष्ट्रवादियों की दिलचस्पी अचानक तथा पूरी तरह से खत्म हो गयी, जो कि दुबारा 1919-22 में ही जागृत हो पायी।
1918 में मजदूर हड़तालों की नयी लहर की शुरुआत होती है। अब होने वाली हड़तालों में मजदूरों की भागीदारी और व्यापक हुई। 1918 में भारत के मजदूर आन्दोलन के इतिहास में बम्बई में पहली आम हड़ताल हुई। इस हड़ताल में 120,000 मजदूर शामिल हुए। इस हड़ताल के समर्थन में देश के अन्य हिस्सों में भी मजदूरों ने हड़तालें कीं। इसके पहले भी फैक्ट्रियों में हड़तालें आम बात थीं, मगर ये कभी भी देशव्यापी नहीं बन पायी थीं। मजदूर हड़तालों की यह देशव्यापी लहर 1921 तक जारी रही, जिसमें बम्बई, मद्रास, असम, पंजाब आदि में सैकड़ों छोटी-बड़ी हड़तालें हुईं, जिनमें लाखों मजदूर शामिल हुए।
1918 की हड़ताल लहर से भारत का मजदूर आन्दोलन एक नये चरण में प्रवेश करता है। अब मजदूरों ने खुद को ट्रेड यूनियनों में संगठित करना शुरू कर दिया। ट्रेड यूनियनें भारत के लिए एक नयी चीज थीं। 1918 के पहले इनका अस्तित्व नहीं था, सिर्फ गोरे मजदूरों की ही चन्द यूनियनें मौजूद थीं (अबनी मुखर्जी, द कम्युनिस्ट रिव्यू, सितम्बर 1922, खण्ड 3, अंक 5)। इसी समय पहली बार बम्बई, मद्रास और कुछ अन्य नगरों में मजदूर संघों की स्थापना हुई। 1920 में मजदूर संघों की प्रतिनिधि और देशव्यापी संस्था ‘आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस’ की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों के हाथों में था।
जिस समय भारत का मजदूर आन्दोलन नये चरण में प्रवेश कर रहा था, उस समय तक आधुनिक मानव इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली घटना घट चुकी थी। वह घटना थी 1917 में रूस में हुई महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति। इस क्रान्ति ने मानव इतिहास में पहली बार शोषित-उत्पीड़ित जनों को मुक्त किया। संसार में पहला मजदूर राज्य अस्तित्व में आया। अक्तूबर क्रान्ति ने पूरे विश्व को झकझोर दिया। अक्तूबर क्रान्ति की बदौलत मजदूर क्रान्ति के विज्ञान, जो कि अब तक मुख्यत: यूरोपीय (तथा उत्तरी अमेरिकी) परिघटना ही था, का प्रकाश अब तीसरी दुनिया के औपनिवेशिक, अर्ध्दऔपनिवेशिक, तथा नव-औपनिवेशिक देशों में भी फैलने लगा। इन देशों में भी अब कम्युनिस्ट पार्टी या संगठन बनने लगे। इसी प्रक्रिया में 17 अक्तूबर 1920 को ताशकंद में एम.एन. राय के नेतृत्व में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। मगर इस पार्टी की भारत की मेहनतकश जनता के बीच कोई जड़ें न थीं। यह ”प्रवासी पार्टी” पत्र व्यवहार, पत्रिकाएँ, घोषणापत्र, तथा दूत व धन भेजकर भारत में कार्यरत राष्ट्रवादियों, मजदूर, किसान नेताओं को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करती रही, जिसमें इसे कोई खास सफलता नहीं मिली। उधर 1921-22 के आसपास इस पार्टी से सर्वथा स्वतन्त्र रूप में भारत में पहले कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे जिनमें एस.ए. डांगे के गिर्द बाम्बे ग्रुप, मुजफ्फर अहमद के गिर्द कलकत्ता ग्रुप, सिंगरावेलु एम. चेट्टियार के गिर्द मद्रास ग्रुप, ग़ुलाम हुसैन के गिर्द लाहौर ग्रुप और कानपुर ग्रुप आदि प्रमुख थे।
सत्यभक्त की पहल पर 25-28 दिसम्बर 1925 में कानपुर में ”प्रथम कम्युनिस्ट सम्मेलन” आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग सक्रिय कम्युनिस्ट ग्रुप एक पार्टी ”भारत की कम्युनिस्ट पार्टी” में एकजुट हुए।
इस सम्मेलन का सकारात्मक पहलू यह था कि इसने देश में बिखरे कम्युनिस्ट ग्रुपों को एकजुट किया। वहीं इसका नकारात्मक पहलू यह था कि यह विचारधारात्मक रूप में अत्यन्त कमजोर थी। (पार्टी की यह कमजोरी बाद के दिनों में भी बनी रही, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे)। ”प्रथम भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन” के आयोजनकर्ता सत्यभक्त कभी भी राष्ट्रवाद से मुक्त नहीं हो पाये। वे खुद को मार्क्सवादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी मानते थे। इसीलिए वह पार्टी का नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रखना चाहते थे। मगर सम्मेलन में वह इस मुद्दे पर किसी का भी समर्थन हासिल नहीं कर सके। अपने इन विचारों के बावजूद वह केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की सदस्य तथा कानपुर प्रोविंशियल सेंटर के सचिव चुने गये। वे अपने ”राष्ट्रवादी कम्युनिज्म” पर अड़े रहे और जल्दी ही सी.पी.आई. से अलग होकर उन्होंने ”राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी” बना ली, जो कुछ ही समय बाद निष्क्रिय हो गयी। दूसरे, इस सम्मेलन ने भारतीय क्रान्ति का कोई सुस्पष्ट कार्यक्रम नहीं अपनाया। तीसरे, इस पार्टी का संगठन लेनिनवादी उसूलों पर आधारित नहीं था। इस मामले में यह पार्टी कुछ ज्यादा ही भारतीय थी। इसी के चलते पार्टी संविधान में ”किसी भी सच्चे मजदूर या किसान” को पार्टी की सर्वोच्च संस्था, यानी वार्षिक सम्मेलन में प्रतिनिधि बनने योग्य ठहराया गया (धारा 6), इसमें प्रान्तीय अथवा यहाँ तक कि जिला कमेटियों को भी ”सदस्यता की शर्तों को नियमबध्द करने का अधिकार दिया गया” (धारा 5 क) तथा पार्टी से सम्बध्द ”मजदूर वर्ग की यूनियनों को” ”सी.पी.आई. का अभिन्न अंग” माना गया (धारा 3 घ)।
औपचारिक तौर पर भले ही देश के अलग-अलग कम्युनिस्ट ग्रुप एक पार्टी में एकजुट हो गये थे, मगर इस पार्टी गठन के बाद भी इसका ढाँचा ढीला और संघात्मक बना रहा और लेनिनवादी अर्थों में इसका नेतृत्वकारी निकाय भी संगठित नहीं था। 1933 में जाकर ही पहली बार पूरी पार्टी एक केन्द्रीय कमेटी के तहत संगठित हो सकी।
बहरहाल, हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के मजदूरों के बीच काम की तरफ लौटते हैं।
1918 से 1921 तक भारत में मजदूर आन्दोलन उफान पर था। 1922 से मजदूर आन्दोलन में उतार का दौर शुरू होता है। लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रह पायी। 1924 से ही फिर से मजदूर आन्दोलन हरकत में आना शुरू होता है। 1924 में बम्बई के टेक्सटाइल मजदूरों का आन्दोलन इसका एक अच्छा उदाहरण है जब यहाँ की 81 मिलों के 1,60,000 मजदूर हड़ताल पर चले गये। 1925 से वर्ग संघर्ष और तीव्र हो गया। मार्च 1925 में उत्तर-पश्चिम रेलवे के मजदूर हड़ताल पर चले गये। इसी वर्ष ”बोनस हड़ताल” नाम से विख्यात बम्बई के टेक्सटाइल मजदूरों का ढाई महीने लम्बा आन्दोलन चला जिसमें 56 हजार मजदूर शामिल थे। 1927 से मजदूर आन्दोलन फिर से पूरे उफान पर था। इसी दौरान भारत के मजदूरों में कम्युनिस्टों का काम शुरु होता है।
”प्रवासी” सी.पी.आई. के काम के तौर-तरीकों की चर्चा हम पहले कर आये हैं। जिसमें वह नेशनल कांग्रेस के नेताओं को अथवा सीधे मजदूर व किसानों के समुदायों के पास घोषणापत्र या अपीलें भेजकर उनकी गतिविधियों को प्रभावित करने की कोशिश करती थी जिसमें उसे खास सफलता नहीं मिली।
भारत में काम कर रहे कम्युनिस्टों ने मजदूर वर्ग के आन्दोलन के विषय में अपने विचार सर्वप्रथम मार्च 1923 के ‘द सोशलिस्ट’ में जाहिर किये थे। ”भारत में पूँजीवादी हमला” शीर्षक एक लेख में केवल सुधारवादी श्रमिक नेताओं की दार्शनिक सलाह सुनने के बदले, जिसे गाँधी के अनुयायी मजदूर मोर्चे पर ”सबकी भलाई” के रूप में प्रचारित करते थे, मजदूरों से पूँजीवादी हमलों के खिलाफ वर्ग संघर्ष छेड़ने की अपील की गयी थी।
1924 में जब कम्युनिस्टों ने मजदूरों में बाकायदा काम की शुरुआत की तो मजदूरों को संगठित करने में प्रयासरत कम्युनिस्ट नेताओं पर शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों ने हमला बोल दिया। एस.ए. डांगे, मुज्ज्फ्फर अहमद और शौकत उस्मानी को 1924 में ही कानपुर बोल्शेविक केस के तहत गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने मजदूरों को संगठित करने की कम्युनिस्टों की शुरुआती पहलकदमी को बुरी तरह झकझोर दिया।
1926-27 के दौरान भारत के विभिन्न राजनीतिक केन्द्रों – जैसे, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, और लाहौर – में मजदूर किसान पार्टियों के उदय से कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं को मजदूरों को संगठित करने में काफी मदद मिली। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में श्रम-सम्बन्धी सवाल उठाकर कांग्रेसी राजनीति में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की। इसी समय में कम्युनिस्टों ने एटक में भी काम शुरू किया। 1927 में सी.पी.आई. की केन्द्रीय कार्यकारिणी की वर्धित सभा ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ”ट्रेड यूनियन कांग्रेस” पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें कम्युनिस्ट सदस्यों का आह्वान किया गया कि वे एटक में घुसकर इस संगठन को इसके मौजूदा बुर्जुआ नेतृत्व के हाथों से छीन लें।
जल्द ही कम्युनिस्टों ने एटक में अपना अच्छा-खासा रसूख कायम कर लिया। 26-27 नवम्बर 1927 को कानपुर में आयोजित एटक की आठवीं कांग्रेस में एक सक्रिय वामपन्थी ग्रुप की उपस्थिति विशेष तौर पर गौरतलब थी।
1928 में मजदूर आन्दोलन में एक नया उभार आया। फरवरी में जिस दिन साइमन कमीशन बम्बई पहुँचा वहाँ एक जोरदार प्रदर्शन हुआ। साइमन कमीशन का विरोध करने 20 हजार मजदूर सड़कों पर उतर आए। दूसरी घटना दिसम्बर में कलकत्ता में हुई। बंगाल की मजदूर किसान पार्टी की रहनुमाई में हजारों मजदूर नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में घुस गए। केन्द्रीय पण्डाल पर कब्जा कर लिया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया। ये दो घटनाएँ भारतीय मजदूरों की बढ़ती साम्राज्यवाद-विरोधी चेतना और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी लगातार बढ़ती भागीदारी को चिह्नित करती थीं। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में मजदूर आन्दोलनों का यह सिलसिला, थोड़े-थोड़े समय के ठहरावों सहित दूसरे विश्व युध्द के शुरू होने तक लगातार चलता रहा। इस अवधि में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर अनेक छोटे-बड़े मजदूर आन्दोलन हुए जिसमें से शोलापुर के टेक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल का जिक़्र यहाँ जरूरी है। 7 मई 1930 को शोलापुर में टेक्सटाइल हड़ताल हुई जो ”शोलापुर कम्यून” के नाम से विख्यात हुई। पूरा शोलापुर शहर 7 से 16 मई तक मजदूरों के नियन्त्रण में चला गया। शहर में मार्शल लॉ लगाने के बाद ही स्थिति ”सामान्य” हो सकी।
इसी समय में एटक में पहली बार फूट (नवम्बर 1929) तथा फिर एकता (अप्रैल 1935) जैसी घटनाएँ भी हुईं।
1939 में दूसरे विश्व युध्द की शुरुआत हुई। युध्द के दौरान सी.पी.आई. ने अपने इतिहास की सर्वाधिक गम्भीर गलतियों में से एक गलती की। 1941 के उत्तरार्ध्द में रूस पर फासीवादी जर्मनी के हमले के बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने फासीवाद विरोधी ”जनयुध्द” को पूर्ण समर्थन देने की लाइन अख्तियार की। भले ही उसने स्वतन्त्रता और तत्काल राष्ट्रीय सरकार के गठन की माँग को भी दोहराया, लेकिन इन माँगों पर कोई देशव्यापी आन्दोलन खड़ा करना उसके एजेण्डे पर नहीं था, क्योंकि वह सोवियत संघ के साथ फासीवाद-विरोधी युध्द में खड़े ब्रिटेन के विरुध्द निर्णायक संघर्ष करके फासीवाद-विरोधी विश्वव्यापी मोर्चे को कमजोर नहीं करना चाहती थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने विश्वस्तर पर प्रधान अन्तरविरोध को ही राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधान अन्तरविरोध मान लिया। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की यह सोच गलत थी। विश्व स्तर के समीकरणों में सोवियत संघ के साथ धुरी शक्तियों के विरुध्द मोर्चा चलाना ब्रिटेन और सभी पश्चिमी साम्राज्यवादियों की मजबूरी थी। आज यह स्थापित सत्य है कि ब्रिटेन और उसके साम्राज्यवादी मित्रों की यह नीति थी कि समाजवाद के सोवियत दुर्ग को फासिज्म की ऑंधी ढहा देगी और इस प्रक्रिया में फासिस्ट ताकतें जब कमजोर पड़ जाएँगी तो उनसे निपट लेंगे। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चर्चिल का कहना था कि अगर हिटलर जीत की तरफ बढ़ेगा तो हम सोवियत संघ का साथ देंगे और अगर सोवियत संघ जीत की तरफ बढ़ेगा तो हम हिटलर का साथ देंगे। यानी साम्राज्यवादियों की नीति इस लड़ाई में इन दोनों को इतना कमजोर करने की थी कि दोनों से आसानी से निपटा जा सके। हिटलर की 200 डिवीजनों से अकेले सोवियत संघ जूझ रहा था लेकिन बार-बार कहने के बावजूद यूरोप में मोर्चा खोलने में बहुत देर की गयी। ऐसी स्थिति में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए और संविधान सभा के लिए आश्वासन लेने और राष्ट्रीय आन्दोलन के कांग्रेसी नेतृत्व के सामने प्रभावी चुनौती प्रस्तुत करने के साथ ही ब्रिटेन पर पश्चिम में भी युध्द का मोर्चा खोलने का दबाव बना सकती थी। वैसे भी, फासीवाद-विरोधी जनयुध्द को भारतीय कम्युनिस्टों के समर्थन से सोवियत संघ को कोई वास्तविक मदद नहीं मिली। जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी फासीवाद-विरोधी मोर्चे को ”मजबूत” बनाने की अपनी अव्यावहारिक गतिविधियों में व्यस्त थी, उसी समय भारतीय बुर्जुआ वर्ग की प्रतिनिधि पार्टी कांग्रेस के नेता युध्द में ब्रिटेन के उलझे होने का तथा इस समय कम्युनिस्टों द्वारा अंग्रेजों के समर्थन की अवस्थिति का फायदा उठाने के बारे में गम्भीरतापूर्वक सोच रहे थे। 1942 के मध्य में स्तालिनग्राद में जर्मन सेना के पाँव उखड़ने लगे। 1942 की गर्मियों में भारतीय बुर्जुआ वर्ग के कुशलतम राजनीतिक प्रतिनिधि और रणनीतिकार गाँधी समझ चुके थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर जनान्दोलन का दबाव बनाकर अधिकतम सम्भव हासिल करने का अनुकूलतम समय आ चुका है। अगस्त 1942 में बम्बई में कांग्रेस के खुले अधिवेशन में गाँधी ने ”करो या मरो” और ”भारत छोड़ो” का नारा देते हुए स्पष्ट कहा कि स्वाधीनता से कम उन्हें कोई भी चीज – कोई भी रियायत मंजूर नहीं है। निश्चय ही ”भारत छोड़ो” आन्दोलन एक देशव्यापी जनउभार था। यह साम्राज्यवाद विरोधी जनभावना की प्रचण्डतम अभिव्यक्ति थी। चोटी के कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी जनसंघर्ष स्वत:स्फूर्त ढंग से जारी रहा और देश के कई अंचलों में महीनों तक आजाद सरकारें काम करती रहीं।
मगर कम्युनिस्ट पार्टी इस प्रचण्ड जनउभार से पूरी तरह कटी रही। मजदूर आन्दोलन के गढ़ बम्बई और कलकत्ता के मजदूर इस आन्दोलन के दौरान काफी हद तक शान्त रहे। कम्युनिस्टों द्वारा इस आन्दोलन के विरोध ने मजदूरों को इस आन्दोलन से दूर रखने में अच्छी-खासी भूमिका निभायी। मजदूर आन्दोलन के इन दो बड़े केन्द्रों में मजदूरों के बीच कम्युनिस्टों का मजबूत आधार था। जहाँ पर कम्युनिस्टों का मजदूरों में प्रभाव नहीं था या कम था, जैसे जमशेदपुर, अहमदाबाद, अहमदनगर, पूना आदि जगहों पर, वहाँ मजदूर बड़े पैमाने पर इस आन्दोलन में कूदे।
1945 के मध्य से मजदूर हड़तालों की एक नयी देशव्यापी लहर आयी। ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक होते जाना इस लहर की विशेषता थी। मजदूर हड़तालें छात्रों और अन्य मेहनतकश समुदायों के राजनीतिक संघर्ष-प्रदर्शनों के साथ जुड़ती जा रही थीं। ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) जनवरी 1945 में मद्रास में हुए 21वें अधिवेशन में ही स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी। 1945 के उत्तरार्ध्द में हड़तालें और प्रदर्शन सेना और पुलिस के साथ सशस्त्र झड़पों और टकरावों की शक्ल लेने लगे थे। 1946 का वर्ष भारत की जनता के चार शौर्यपूर्ण संघर्षों का साक्षी बना। 18 से 23 फरवरी 1946 के बीच बम्बई में नौसेना विद्रोह हुआ, जो राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के इतिहास की एक युगान्तरकारी घटना थी, जिसके वास्तविक महत्व का इतिहासकारों ने अभी तक बहुत कम आकलन किया है। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में सितम्बर 1946 में तेभागा आन्दोलन शुरू हुआ। बंगाल का तेभागा आन्दोलन असामी काश्तकारों और बटाईदारों (बरगादारों और अधियारों का आन्दोलन था।) उनकी माँग थी कि जोतदारों को दिया जाने वाला लगान उपज का एक तिहाई होना चाहिए। जंगल की आग की तरह यह आन्दोलन सितम्बर 1946 में शुरू होकर जल्दी ही बंगाल के 11 जिलों में फैल गया। इसमें भाग लेने वाले किसानों की संख्या 50 लाख तक जा पहुँची।
अक्तूबर 1946 में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में सुप्रसिध्द पुनप्रा-वायलार का किसान आन्दोलन हुआ। पुनप्रा और वायलार उत्तरी-पश्चिमी त्रावणकोर के शेरतलाई-अलेप्पी-अम्बालपुझा क्षेत्र के दो गाँव हैं, जिन्हें शौर्यपूर्ण किसान संघर्षों के दौरान हुई शहादतों ने अमर बना दिया।
जुलाई 1946 से अक्तूबर 1951 के बीच आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान छापामार संघर्ष हुआ। तेलंगाना संघर्ष का फलक तेभागा और पुनप्रा-वायलार से काफी बड़ा था। अपने चरम पर इस सशस्त्र संघर्ष ने कुल 3 हजार गाँवों के 16 हजार वर्गमील क्षेत्र को मुक्त करा लिया था। यहाँ पर एक बार फिर हमें कम्युनिस्ट पार्टी की ऐतिहासिक चूक देखने को मिलती है। नौसैना विद्रोह की खबर मिलते ही, पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने पहलकदमी लेकर उसे राजनीतिक नेतृत्व देने की कोशिश नहीं की, जबकि लीग और कांग्रेस द्वारा इस विद्रोह के विरोध का रुख देखते हुए हालात अनुकूल थे। इस विद्रोह के समर्थन में केवल बम्बई में हड़ताल से आगे बढ़कर कम्युनिस्ट पार्टी यदि पूरे देश में आम राजनीतिक हड़ताल का आह्नान करती तो स्थितियाँ एक आम बगावत तक जा सकती थीं। यदि यह आम बगावत सफल नहीं होती, तो पीछे हटकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनयुध्द की नीति अपनाते हुए किसान संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए पार्टी देशव्यापी विद्रोह के अगले चक्र का इन्तजार कर सकती थी। नौसेना (और सेना-वायुसेना में भी सम्भावित) विद्रोह से उसे जनता को सशस्त्र करने के अनुकूल अवसर मिल सकते थे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का नेतृत्व कम्युनिस्टों के हाथ में आ जाना लगभग तय था। मगर ऐसा न हो सका। इसी तरह पार्टी तेभागा, पुनप्रा-वायलार-तेलंगाना के किसान संघर्षों को भी दीर्घकालिक जनयुध्द की राह पर आगे नहीं बढ़ा पायी। 1946 से लगभग 1950 तक जारी संक्रमण काल का वह कोई लाभ नहीं उठा सकी। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी की एक के बाद एक चूकों की जड़ इस बात में थी कि यह पार्टी विचारधारात्मक रूप से अत्यन्त कमजोर थी।
यह निर्विवाद है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में मेहनतकशों की मुख्य भूमिका रही और इन्हीं के दम पर यह लड़ाई लड़ी गयी। ब्रिटिश भारत के दो ही वर्ग ऐतिहासिक तौर पर इस लड़ाई को नेतृत्व देने के योग्य थे – भारतीय पूँजीपति वर्ग और भारतीय सर्वहारा वर्ग। भारतीय पूँजीपति वर्ग ने खुद को सबसे पहले संगठित किया, आजादी की लड़ाई में अपना नेतृत्व स्थापित किया और उसे अन्त तक बनाये रखने में सफल रहा।
ठीक इसके विपरीत सबसे क्रान्तिकारी वर्ग होते भी मजदूर वर्ग अपने को देर से संगठित कर पाया। इसकी पार्टी देर से अस्तित्व में आयी। सर्वाधिक क्रान्तिकारी वर्ग होने के कारण और शोषणविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना के अपने लक्ष्य के चलते इसे ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसकी असफलता का मुख्य कारण इसकी आत्मगत कमजोरियाँ थीं। इसका नेतृत्व मार्क्सवाद को आत्मसात करने और देश की ठोस परिस्थितियों से उसे मिलाने में असफल रहा। इसकी कुछ और चर्चा हम आगे चलकर करेंगे।
बहरहाल, आइए हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मजदूर वर्ग के बीच काम की अपनी मूल चर्चा पर लौटें। 1923 के बाद से, जब से कम्युनिस्टों ने भारत के मजदूर वर्ग में काम शुरू किया, कम्युनिस्टों के नेतृत्व में आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर अनेक छोटे तथा बड़े मजदूर आन्दोलन हुए। इस पूरी अवधि (1951 तक, जब कम्युनिस्ट पार्टी तेलंगाना संघर्ष को वापस लेकर संशोधनवाद की डगर पर चल पड़ी) भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन का इतिहास जुझारू संघर्षों, शौर्य और पराक्रम, त्याग और कुर्बानियों का रक्तरंजित इतिहास रहा है।
वहीं इस स्थिति का दूसरा पहलू यह है कि 1951 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मजदूर वर्ग में काम अर्थवादी भटकाव का शिकार रहा। मजदूर वर्ग में आर्थिक काम और राजनीतिक काम तथा पार्टी कार्य तथा जनकार्य में तालमेल बिठाने में भी समस्याएँ रहीं। पार्टी ने मजदूर वर्ग की राजनीतिक शिक्षा पर पूरा ध्यान नहीं दिया और न ही व्यापक मजदूर आबादी में राजनीतिक-विचारधारात्मक प्रचार-प्रोपेगैंडा के कोई प्रयास किये। उक्त अवधि में पार्टी ने कई पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित कीं जैसे कि अंग्रेजी में ‘नेशनल फ्रण्ट’, ‘न्यू एज’, बंगला में ‘गणशक्ति’, मलयालम में ‘प्रभातम’, मराठी में ‘क्रान्ति’, तेलुगू में ‘नवशक्ति’ और तमिल में ‘जनशक्ति’। लेकिन पार्टी ने वर्ग-सचेत मजदूरों को सम्बोधित ‘इस्क्रा’ जैसा कोई मजदूर अखबार नहीं निकाला, जो मजदूर वर्ग में सीधे मार्क्सवाद-लेनिनवाद का प्रचार करे, मजदूर वर्ग को उसके ऐतिहासिक मिशन से परिचित कराये। ”जो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन के सभी रणकौशलात्मक, राजनीतिक और सैध्दान्तिक समस्याओं पर ध्यान दे” (लेनिन), जो मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक, और आह्नानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी संगठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भूमिका निभाये। न ही पार्टी के पास व्यापक मजदूर आबादी को सम्बोधित ‘प्रावदा’ जैसा ही कोई अखबार था। संक्षेप में कहें तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूर वर्ग में काम करने के लिए लेनिनवादी पद्धति का अनुसरण नहीं किया। भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन में ‘इस्क्रा’ जैसे किसी अखबार की अवधारणा तो सिरे से गैरहाजिर थी।
लेनिन कहते हैं, ”सामाजिक-जनवाद (यानी कम्युनिज्म) मजदूर आन्दोलन और समाजवाद का मेल है। उसका काम मजदूर आन्दोलन की हर अलग-अलग अवस्था में निष्क्रिय रूप से उसकी सेवा करना नहीं, बल्कि पूरे आन्दोलन के हितों का प्रतिनिधित्व करना, इस आन्दोलन को उसके अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचाना तथा उसके राजनीतिक और विचारधारात्मक स्वतन्त्रता की रक्षा करना है। सामाजिक जनवाद से कटकर मजदूर आन्दोलन अनिवार्य रूप में पूँजीवादी बन जाता है।… हमारा मुख्य और मूल काम मजदूर वर्ग के राजनीतिक विकास और राजनीतिक संगठन के कार्य में सहायता पहुँचाना है। इस काम को जो लोग पीछे धकेल देते हैं, जो तमाम विशेष कामों और संघर्ष के विशिष्ट तरीकों को इस मुख्य काम के अधीन बनाने से इनकार करते हैं, वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं और आन्दोलन को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं।” (लेनिन, सम्पूर्ण ग्रन्थावली, खण्ड 4, पृष्ठ 367-69)
मगर हमारे यहाँ पार्टी ने मजदूर आन्दोलन और समाजवाद के संयोजन के कोई प्रयास नहीं किये, मजदूर वर्ग में उसकी विचारधारा मार्क्सवाद-लेनिनवाद का वर्चस्व स्थापित करने के प्रयास नहीं किये और मजदूर वर्ग में पूँजीवादी विचारधारा के वर्चस्व का रास्ता साफ कर दिया। यही वजह थी कि जहाँ-जहाँ मजदूर वर्ग में कम्युनिस्ट पार्टी का मजबूत आधार था वहाँ भी शत्रु वर्ग मजदूर वर्ग में सेंध लगाने में कामयाब होते रहे और यहाँ तक कि साम्प्रदायिक शक्तियाँ तक मजदूरों को भरमाने, बहकाने, साम्प्रदायिक फसादों में झोंक देने में कामयाब होती रहीं। 1945 में मजदूर आन्दोलन में नया उभार आया और कम्युनिस्ट नेतृत्व में मजदूरों के जुझारू आन्दोलन आगे बढ़ने लगे। इस जुझारू एकता को तोड़ने के लिए साम्राज्यवादी हुक्मरानों ने साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिशें कीं। कम्युनिस्टों की अगुवाई में मजदूर आन्दोलन के सबसे मजबूत गढ़ बम्बई में वह अपनी कोशिश में कामयाब भी हुए। तेभागा किसान आन्दोलन के समर्थन में सी.पी.आई. ने 28 मार्च 1947 को आम हड़ताल की योजना बनायी थी। मगर इसी समय बंगाल में बँटवारे के लिए हिन्दू महासभा का अभियान भी जोर पकड़ रहा था, 27 मार्च से कलकत्ता में साम्प्रदायिक फसाद शुरू हो गए, जिसने शहरों में तेभागा आन्दोलन के समर्थन में किसी भी तरह की कार्रवाई की तमाम सम्भावनाएँ खत्म कर दीं।
मजदूरों के बीच कम्युनिस्ट पार्टी के कामों की जो कमजोरियाँ रही हैं, पार्टी की अन्य तमाम गलतियों-कमजोरियों की तरह उनका मूल कारण भी पार्टी की विचारधारात्मक कमजोरी ही रहा है। इस कमजोरी के कारण ही, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, उस दौर में भी, जबकि वह संशोधनवाद के दलदल में नहीं जा धँसी थी और बुनियादी तौर पर इसका चरित्र सर्वहारा वर्गीय था, कभी भी संगठन के बोल्शेविक उसूलों के अनुरूप इस्पाती साँचे में ढली और जनवादी केन्द्रीयता पर अमल करने वाली पार्टी के रूप में काम नहीं करती रही थी। पार्टी-गठन के बाद लम्बे समय तक इसका ढाँचा ढीला-ढाला था और लेनिनवादी तरीके से इसका नेतृत्वकारी निकाय भी संगठित नहीं था। पहली बार ब्रिटेन, जर्मनी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों के एक संयुक्त पत्र (मई, 1932), ”इन्प्रेकोर” में प्रकाशित एक लेख (फरवरी-मार्च, 1933), और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक और पत्र (जुलाई, 1933) द्वारा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के ग्रुपों में बिखरे होने, गैर-बोल्शेविक ढाँचा तथा कार्यप्रणाली विषयक कार्यभारों की उपेक्षा की आलोचना करने और आवश्यक सुझाव दिये जाने के बाद दिसम्बर 1933 में सी.पी.आई. की अस्थाई कमेटी के केन्द्रक का गठन हुआ, जिसे कुछ और लोगों को सहयोजित करने के बाद केन्द्रीय कमेटी का नाम दे दिया गया। इसके बाद ढाई वर्षों तक पार्टी महासचिव का पद कामचलाऊ प्रबन्ध के तहत कोई न कोई सम्भालता रहा। अप्रैल, 1936 में पी.सी. जोशी के महासचिव चुने जाने के बाद यह स्थिति समाप्त हो सकी। लेकिन इसके बाद भी पार्टी के बोल्शेविकीकरण की प्रक्रिया को कभी भी सहज ढंग से अंजाम नहीं दिया गया। पी.सी. जोशी के नेतृत्वकाल वाले दक्षिणपन्थी भटकाव के दौर में, पार्टी सदस्यता की शर्तों, कमेटी व्यवस्था और गुप्त ढाँचे के मामले में बहुत ही अधिक ढिलाई-लापरवाही बरती जाती थी जो 1942 में पार्टी के कानूनी घोषित किये जाने पर और अधिक बढ़ गयी। उल्लेखनीय है कि पार्टी की पहली कांग्रेस भी उसके कानूनी घोषित किए जाने के बाद ही जाकर (23 मई-1 जून, 1943, बम्बई) सम्भव हो सकी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत के कम्युनिस्ट राज्यसत्ता के दमन एवं गैरकानूनी होने की स्थितियों में पार्टी के सुचारु संचालन के लिए बोल्शेविकों और अन्य दक्ष लेनिनवादी पार्टियों की तरह तैयार नहीं थे। 1936 से लेकर 1948 तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पर इसके महासचिव पी.सी. जोशी की दक्षिणपन्थी लाइन हावी रही। 1948 में जब पी.सी. जोशी की जगह बी.टी. रणदीवे पार्टी के महासचिव बने तो पार्टी का पेण्डुलम दूसरे छोर पर जा पहुँचा और पार्टी पर बी.टी. रणदीवे की ”वामपन्थी” दुस्साहसवादी लाइन हावी हो गयी। इन दोनों लाइनों ने भारत के मजदूर आन्दोलन को पर्याप्त नुकसान पहुँचाया। एक जनवादी केन्द्रीयता वाले बोल्शेविक ढाँचे के काफी हद तक अभाव के चलते, दो लाइनों के संघर्षों के सुसंगत संचालन का पार्टी में सदा अभाव रहा। ”वामपन्थी” और दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्तियों का सहअस्तित्व पार्टी में हमेशा बना रहा। कभी एक तो कभी दूसरी लाइन पार्टी पर हावी होती रही और कभी दोनों की विचित्र खिचड़ी पकती रही। संकीर्ण गुटवाद की प्रवृति केन्द्रीय कमेटी के गठन के बाद भी, हर स्तर पर मौजूद रही। दरअसल पार्टी नेतृत्व ने पार्टी निर्माण को कभी एक महत्वपूर्ण कार्यभार माना ही नहीं। कतारों की विचारधारात्मक-राजनीतिक-व्यावहारिक शिक्षा के जरिये बोल्शेविकीकरण और दोष-निवारण पर कभी जोर नहीं दिया गया।
अपने विचारधारात्मक दिवालियेपन के चलते भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व ने औपनिवेशिक भारत के उत्पादन-सम्बन्धों और अधिरचना के सभी पहलुओं (जिनमें जाति व्यवस्था, स्त्री प्रश्न और राष्ट्रीयताओं का प्रश्न भी आता है) का ठोस अध्ययन करके भारतीय क्रान्ति की रणनीति एवं आम रणकौशल के निर्धारण की कोई स्वतन्त्र कोशिश दरअसल की ही नहीं और अन्तरराष्ट्रीय नेतृत्व और बड़ी बिरादर पार्टियों के आकलनों के हिसाब से ही हमेशा निर्णय लेता रहा। ऐसी स्थिति में संयुक्त मोर्चा, मजदूर आन्दोलन और अन्य प्रश्नों पर पार्टी बार-बार दो छोरों के भटकाव का शिकार होती रही। जाहिर है ऐसे में अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में समय-समय पर पैदा होने वाले विचलन और भारत-विषयक गलत या असन्तुलित मूल्यांकन भी भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन को प्रभावित करते रहे।
यह पार्टी की विचारधारात्मक कमजोरी और नेतृत्व की बौध्दिक अक्षमता-विपन्नता ही थी, जिसके कारण भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद की सार्वजनीन सच्चाइयों को भारत की ठोस परिस्थितियों में लागू करने में हमेशा ही विफल रही, बल्कि ऐसा प्रयास तक करने के बजाय हमेशा ही अन्तरराष्ट्रीय नेतृत्व और बड़ी एवं अनुभवी बिरादर पार्टियों का मुँह जोहती रही। ज्यादातर कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल के प्रस्तावों-सर्कुलरों, उसके मुखपत्रों में प्रकाशित लेखों, सोवियत पार्टी के लेखों और ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के रजनीपाम दत्त जैसे लोगों के प्रभाव में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी नीतियाँ और रणनीति तय करती रही। इससे अधिक त्रासद विडम्बना भला और क्या हो सकती है कि 1951 तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के पास भारतीय क्रान्ति का कोई कार्यक्रम तक नहीं था, केवल कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल द्वारा प्रवर्तित आम दिशा और दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिखे कुछ निबन्ध, प्रस्ताव और रणकौशल एवं नीति-विषयक दस्तावेज मात्र ही थे जो बताते थे कि भारत में राष्ट्रीय जनवादी क्रान्ति का कार्यभार सम्पन्न करना है। मुख्यत: भूमि क्रान्ति का कार्यभार होने के बावजूद कोई भूमि कार्यक्रम तैयार करना तो दूर, भूमि-सम्बन्धों की विशिष्टताओं को जानने-समझने के लिए कभी कोई विस्तृत जाँच-पड़ताल तक नहीं की गयी थी। ऐसी स्थिति के होते हुए, यदि पार्टी राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की नेतृत्वकारी शक्ति नहीं बन सकी, अनुकूल स्थितियों का लाभ उठाने से बार-बार चूकती रही और जनसंघर्षों में कम्युनिस्ट कतारों की साहसिक भागीदारी और अकूत कुर्बानियाँ व्यर्थ हो गयीं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहली बार पार्टी नेतृत्व ने, अपने एक प्रतिनिधिमण्डल की स्तालिन और सोवियत पार्टी के अन्य नेताओं से वार्ता के बाद, 1951 में एक कार्यक्रम और नीति-विषयक वक्तव्य तैयार करके जारी किया जिसे अक्तूबर, 1951 में पार्टी के अखिल भारतीय सम्मेलन और फिर दिसम्बर, 1953 में तीसरी पार्टी कांग्रेस में पारित किया गया।
1951 में ही पार्टी संसदवाद, संशोधनवाद की राह की राही हो गयी थी और मुख्यत: और मूलत: मेंशेविक और काउत्स्कीपन्थी यूरोपीय पार्टियों के साँचे में ढल चुकी थी। 1951 से लेकर 1962-63 तक इसमें दो लाइनों का संघर्ष वस्तुत: संसदवाद-अर्थवाद की नरम धारा और रैडिकल धारा के बीच संघर्ष के रूप में मौजूद था। कतारों का बड़ा हिस्सा क्रान्तिकारी आकांक्षाओं और चरित्र वाला था, लेकिन अपनी विचारधारात्मक कमजोरी के कारण रैडिकल संशोधनवादी धड़े को क्रान्तिकारी मानता था। पार्टी में उक्त दो लाइनों के संघर्ष का परिणाम था 1964 की फूट और नयी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का गठन। इस फूट का मुख्य मुद्दा विचारधारात्मक-राजनीतिक नहीं था, बल्कि संसदीय राजनीति में अधिक नरम या अधिक गरम नीतियों-रणनीतियों को लेकर था। नवगठित पार्टी सी.पी.आई. (एम) अपने जन्म से ही एक संशोधनवादी पार्टी थी। इस पर और अधिक चर्चा करना वक्त की बर्बादी होगी।
नक्सलबाड़ी का किसान विद्रोह –
भारत में एक नयी कम्युनिस्ट धारा का उदय और बिखराव
मई 1967 में पश्चिम बंगाल के तराई अंचल नक्सलबाड़ी में एक ऐतिहासिक किसान विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसने आजाद भारत के नये हुक्मरानों को कँपकँपा दिया। नक्सलबाड़ी से भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन ने एक नये दौर में प्रवेश किया। देश के कोने-कोने में नक्सलबाड़ी का झण्डा बुलन्द करने वाले हजारों कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों ने खुद को सी.पी.आई. (एम) से अलग कर लिया। इस तरह उन्होंने सी.पी.आई. तथा सी.पी.आई. (एम) के संशोधनवाद तथा नवसंशोधनवाद से निर्णायक विच्छेद किया। नक्सलबाड़ी ने भारत की शोषित-उत्पीड़ित मेहनतकश जनता के अन्दर मुक्ति की एक नयी आशा का संचार किया।
लेकिन भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन के जन्म से ही जो विचारधारात्मक कमजोरी इसका पीछा करती रही है, नक्सलबाड़ी से पैदा हुई कम्युनिस्टों की नयी धारा भी इस कमजोरी से मुक्त नहीं थी। नक्सलबाड़ी के क्रान्तिकारी भी विचारधारात्मक दिवालियेपन तथा बौध्दिक विपन्नता की परम्परा के बोझ तले दबे हुए थे। भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन की शुरुआत से ही अन्तरराष्ट्रीय नेतृत्व पर जो निर्भरता बनी रही थी, वह अब भी जारी थी। पहले भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अपने हर छोटे-बड़े फैसले के लिए सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य बड़ी बिरादर पार्टियों का मुँह जोहती थी, अब नक्सलबाड़ी से जो नयी कम्युनिस्ट धारा पैदा हुई वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुँह जोहने लगी। नक्सलबाड़ी के क्रान्तिकारियों में चीनी क्रान्ति की हूबहू नकल करने की प्रवृति हावी थी। उन्होंने भारत की ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण किए बिना भारतीय समाज को अर्ध्द-सामन्ती, अर्ध्द-औपनिवेशिक घोषित कर दिया और कहा कि भारतीय क्रान्ति का मार्ग दीर्घकालिक जनयुध्द का मार्ग होगा।
भारतीय समाज का यह ”विश्लेषण” उस समय के भारत की जमीनी सच्चाइयों से कोसों दूर था। 1967 तक आते-आते भारतीय समाज पूँजीवादी विकास का दूसरा चरण पूरा कर चुका था (अगर औपनिवेशिक भारत में जो पूँजीवादी विकास हुआ था उसको भारत में पूँजीवादी विकास का पहला चरण मानें तो)। 1947 में सत्ता हस्तान्तरण के बाद भारत की राजनीतिक सत्ता पर यहाँ का बुर्जुआ वर्ग काबिज हुआ। उसने ऊपर से धीमे आर्थिक सुधारों के जरिये भारत में पूँजीवादी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 1967 तक आते-आते भारत के सामाजिक-आर्थिक हालात बहुत ही विविधतापूर्ण थे। कुछ इलाकों में पूँजीवादी विकास काफी आगे बढ़ गया था, कहीं सामन्ती उत्पादन सम्बन्धों की जकड़ बहुत मजबूत थी, कहीं पर सामन्ती अवशेष काफी प्रबल थे। इस विविधतापूर्ण तथा संक्रमणशील सामाजिक यथार्थ को समझना नेतृत्व से बहुत परिपक्वता तथा गहरी विचारधारात्मक समझ की अपेक्षा करता था। लेकिन नक्सलबाड़ी से जो नया कम्युनिस्ट नेतृत्व पैदा हुआ वह ऐसा नहीं था। उसमें परिपक्वता तथा विचारधारात्मक समझदारी का नितान्त अभाव था।
नक्सलबाड़ी का किसान विद्रोह एक जनान्दोलन था जिसके नेता कानू सान्याल, खोकन मजुमदार, कदम मलिक तथा जंगल संथाल आदि थे जिन्होंने जनदिशा पर अमल करते हुए इस आन्दोलन को निर्मित किया था। राजनीतिक तथा विचारधारात्मक मार्गदर्शन के रूप में चारु के आठ दस्तावेजों की भी इस आन्दोलन के निर्माण में एक हद तक की भूमिका रही थी। चारु मजुमदार अपने आठ दस्तावेजों के लेखन के समय से ही एक सुसंगत ”वाम” आतंकवादी लाइन के पक्षधर तथा प्रस्तोता थे। जिस समय नक्सलबाड़ी में जनान्दोलन तूफानी गति से आगे बढ रहा था उसी समय चारु की ”वाम” आतंकवादी लाइन नक्सलबाड़ी के पास ही के इलाके इसलामपुर-चतरहाट में बुरी तरह पिट चुकी थी। नक्सलबाड़ी का जनान्दोलन जब एक जगह जाकर ठहराव का शिकार हो गया तो इसके नेतृत्व ने अपनी विचारधारात्मक कमजोरियों के चलते चारु की आतंकवादी लाइन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ ही समय में चारु की आतंकवादी लाइन ने नक्सलबाड़ी के महान जनान्दोलन को तबाह कर दिया। बाद में भी चारु की आतंकवादी लाइन ने कई जनान्दोलनों को तबाह किया जिसमें श्रीकाकुलम के गिरिजनों का आन्दोलन, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के देबरा और गोपीवल्लभपुर का किसान आन्दोलन, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी अंचल के किसानों का आन्दोलन, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के तराई अंचल के किसानों का आन्दोलन आदि प्रमुख हैं।
नक्सलबाड़ी के किसान विद्रोह के बाद सी.पी.आई. (एम) से बाहर आये कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों ने खुद को भारत के कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की अखिल भारतीय तालमेल कमेटी में संगठित किया। इस कमेटी ने अपने आगे अन्य कई कार्यभारों के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण कार्यभार यह रखा कि कमेटी माओ त्से-तुङ विचारधारा की रोशनी में भारतीय परिस्थिति के सुनिश्चित विश्लेषण के आधार पर क्रान्तिकारी कार्यक्रम और रणकौशल तैयार करेगी। मगर तालमेल कमेटी पर चारु की लाइन के हावी होने के कारण भारतीय परिस्थिति के विश्लेषण का काम कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के एजेण्डे पर न आ सका। बाद में चारु मजुमदार ने बेहद नौकरशाहाना तरीके से तालमेल कमेटी से ”आन्ध्र प्रदेश कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कमेटी” को बाहर निकाल दिया तथा 22 अप्रैल 1969 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के गठन की घोषणा कर दी।
”वामपन्थी” आतंकवादी लाइन के प्रस्तोता चारु मजुमदार ने कई नायाब सिध्दान्त प्रतिपादित किये। उन्होंने जनता के हर तरह के जनसंगठनों तथा आर्थिक संघर्षों को अर्थवाद, सुधारवाद कहकर क्रान्ति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ग-शत्रु का सफाया वर्ग संघर्ष का सर्वोच्च रूप है। चारु की यह ”वाम” आतंकवादी लाइन एक के बाद एक जगह बार-बार पिटती रही। लेकिन एक नये प्रयोग के लिए इसे कोई दूसरी जगह मिल जाती थी।
औद्योगिक मजदूरों से इस आतंकवादी लाइन का कुछ लेना-देना नहीं था क्योंकि शहरों तथा अन्य औद्योगिक केन्द्रों पर यह लाइन नहीं चल सकती थी। औद्योगिक मजदूरों के लिए भी इस लाइन पर करने के लिए कुछ खास नहीं था। यह लाइन अपने व्यवहार के लिए सुदूर, दुर्गम पिछड़े इलाकों की तलाश में रहती थी। उस समय भारत में ऐसे कई अंचल मिल जाते थे और भारत के पूँजीवादी विकास के पिछड़ेपन के चलते आज भी ऐसे बेहद पिछड़े कई इलाके मौजूद हैं। आज ऐसी जगहों पर थोड़े फेरबदल के साथ चारु की आतंकवादी लाइन को भाकपा (माओवादी) लागू कर रही है। शहरों में तो पहले से ही इस आतंकवादी लाइन के लागू होने की जमीन नहीं थी, मगर अब पिछले छह दशकों के पूँजीवादी विकास ने ग्रामीण मैदानी इलाकों से भी इस लाइन के व्यवहार की जमीन खत्म कर दी है। इसीलिए आज भाकपा (माओवादी) बेहद पिछड़े जंगली इलाके में सिमटी हुई है जहाँ बेहद पिछड़ी चेतना वाली आदिवासी आबादी में इसका जनाधार बना है, क्योंकि वहीं पर ही ऐसा सम्भव है। यह पार्टी इस जंगली इलाके में मुक्त क्षेत्र बनाने का सपना देख रही है। यह पार्टी सपना देख रही है कि एक दिन इसकी लाल सेना इन जंगलों से बाहर निकलेगी, पहले ग्रामीण मैदानी इलाकों, फिर कस्बों तथा अन्त में बड़े शहरों पर कब्जा करते हुए एक दिन पूरे देश पर कब्जा कर लेगी और क्रान्ति हो जायेगी। आज के भारत में इस सपने के सच हो सकने की सम्भावना पर कोई अहमक ही विश्वास कर सकता है। मगर हमारे देश की मिट्टी को कुछ अजब वरदान है कि ऐसे सपनों में विश्वास रखने वालों की भी यहाँ कमी नहीं है।
जिन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी ग्रुपों ने चारु की आतंकवादी लाइन का विरोध किया था तथा जनदिशा की वकालत की थी, वे ग्रुप भी लगातार टूट-बिखराव का शिकार रहे हैं। इसमें से कई तो विसर्जित हो चुके हैं। कुछ इसी नियति की ओर अग्रसर हैं। बाकी जो बचे हैं वे पिछले चार दशकों से ग्रामीण मजदूरों तथा किसानों में काम करते आ रहे हैं। ग्रामीण मजदूरों में ये अर्थवादी तरीके से मजदूरों के आर्थिक संघर्ष लड़ने के साथ-साथ, उनमें सम्पत्ति (जमीन) की भूख जगाने के प्रतिक्रियावादी क्रियाकलापों में लिप्त रहते हैं। किसानों में ये फसलों के लाभकारी मूल्य तथा लागत मूल्य में कमी के संघर्ष लड़ते हुए धनी किसानों का मुनाफा बढ़वाने में व्यस्त रहते हैं।
इन ग्रुपों ने नयी जनवादी क्रान्ति को भी कुछ अजीबोगरीब ढंग से समझा है। जब चारु ने यह नारा दिया था कि ”चीन का रास्ता हमारा रास्ता” तो वह भूल गये थे कि चीन की क्रान्ति वाम और दक्षिण भटकावों से सतत लड़ते हुए, जनदिशा पर अमल करते हुए कामयाब हुई थी। नक्सलबाड़ी के समय कहा गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी ग्राम आधारित पार्टी होगी। नयी जनवादी क्रान्ति को किसानों में काम करने तक घटा दिया गया। जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिसने अक्तूबर 1949 में अपने देश में सफल नयी जनवादी क्रान्ति की थी, शुरू से ही औद्योगिक मजदूरों में काम करती रही थी तथा बाद के दौरों (1949) तक उसका औद्योगिक मजदूरों में मजबूत आधार बना रहा था।
नयी जनवादी क्रान्ति की इस विकृत समझ के चलते हमारे देश के माले ग्रुपों ने या तो औद्योगिक मजदूरों में काम किया ही नहीं, और अगर कहीं किया भी तो सी.पी.आई., सी.पी.आई. (एम) के अर्थवाद, ट्रेड यूनियनवाद के बरक्स उन्होंने जुझारू अर्थवाद तथा जुझारू ट्रेड यूनियनवाद का मॉडल ही प्रस्तुत किया। उन्होंने कहीं भी मजदूरों में लेनिनवादी शैली में काम नहीं किया।
इन ग्रुपों ने दूसरे विश्वयुध्द के बाद देश तथा दुनिया में हुए परिवर्तनों से पूरी तरह ऑंखें मूँद रखी हैं। इनके लिए आज भी दुनिया वहीं खड़ी है जहाँ दूसरे विश्वयुध्द के समय थी। इनके लिए दुनिया 1945 में ही ठहर गयी है। मगर यह तो एक भ्रम है। दरअसल दुनिया आगे बढ़ गई, ये ग्रुप 1945 में ठहर गये हैं।
पिछले छह दशकों में भारत में हुआ पूँजीवादी विकास अब सुस्पष्ट रूपरेखा अख्तियार कर चुका है। मगर इन ग्रुपों के लिए तो भारत अब भी अर्ध्द-सामन्ती, अर्ध्द-औपनिवेशिक है। लेकिन ऐसा भारत केवल इनकी कल्पनाओं में ही बसता है, हकीकत में नहीं। मगर कल्पनाओं का भी तो कोई भौतिक आधार होता है। ये ग्रुप बिना किसी भौतिक आधार के किस तरह कल्पना कर लेते हैं, यह एक गहरा रहस्य है जिसका उद्धाटन सिर्फ ये ग्रुप ही कर सकते हैं।
इन ग्रुपों की नयी जनवादी क्रान्ति की गाँठ कुछ इस कदर उलझ गयी है कि खुल नहीं पा रही है। क्योंकि यह खुल नहीं रही है इसलिए ज्यादातर ग्रुपों ने इसे खोलने की कोशिश ही छोड़ दी है।
भारत में नयी जनवादी क्रान्ति के कार्यक्रम को मानने वाले ग्रुपों में से सबसे बड़ा ग्रुप भाकपा (माओवादी) सुदूर जंगलों में आतंकवादी लाइन लागू कर रहा है। बाकी ग्रुप एकदम खुले ढाँचे वाले संगठन चलाए हुए हैं। जनान्दोलनों के नाम पर कुछ न कुछ अर्थवादी कवायद करते रहते हैं। कुछ ग्रुपों के सांगठनिक ढाँचे तो सी.पी.आई. (एम) के संशोधनवादियों से भी गए-गुजरे हैं।
दूसरे विश्वयुध्द के बाद साम्राज्यवाद की कार्यप्रणाली तथा पूँजीवाद की आन्तरिक सरंचना में बहुत बड़े परिवर्तन आये हैं। आज परिस्थितियाँ बेहद जटिल हो गयी हैं जिन्हें समझकर अब कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों को नयी राह खोजनी है। मगर हमारे यहाँ के माले ग्रुप तो बनी-बनायी राह को भी ठीक से नहीं समझ पाये। इनकी तो नयी जनवादी क्रान्ति की भी ठीक समझदारी नहीं बन पायी। आज की जटिल परिस्थितियों को समझने तथा इसमें नयी राह खोजने की तो इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। जिनको आज भी भारत में सामन्तवाद नजर आता है, उनसे और कुछ भी देख सकने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मगर हमारे ये क्रान्तिकारी बिरादर हैं बहुत जिद्दी। इनकी जिद है कि बदली हुई सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की ऐसी की तैसी, हम तो नयी जनवादी क्रान्ति ही करेंगे। इनकी इस जिद को ”सलाम” करते हुए इनकी चर्चा यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं।
आज का मजदूर आन्दोलन : नयी चुनौतियाँ, नयी सम्भावनाएँ
विश्व स्तर पर देखें तो पिछली सदी में मजदूर क्रान्तियों को जो पराजय झेलनी पड़ी, उस पछाड़ (सेटबैक) से मजदूर आन्दोलन अभी भी उभर नहीं पाया है। आज भी पूरी दुनिया में क्रान्ति पर प्रतिक्रान्ति की लहर हावी है। दूसरे, विश्व स्तर पर साम्राज्यवाद की कार्यप्रणाली तथा पूँजीवाद की आन्तरिक संरचना में कई बदलाव आए हैं। बीसवीं सदी में मजदूर क्रान्तियों की पराजय के बुनियादी कारणों तथा आज की दुनिया में आए परिवर्तनों को समझे बगैर मजदूर आन्दोलन का अग्रवर्ती विकास नामुमकिन है। आज विश्व सर्वहारा के पास न तो कोई समाजवादी देश ही बचा है न ही कोई अनुभवी, परिपक्व नेतृत्व ही है जिसके चलते मजदूर वर्ग के लिए परिस्थितियाँ अधिक कठिन तथा चुनौतीपूर्ण हो गयी हैं। मगर इस परिस्थिति का दूसरा पहलू यह है कि कम्युनिस्ट सफल क्रान्तियों की नकल करने तथा अन्तरराष्ट्रीय नेतृत्व का मुँह जोहने की प्रवृति से मुक्त हो सकते हैं क्योंकि आज ऐसा नेतृत्व है ही नहीं। इसीलिए अब तो अपनी राह खुद ही बनानी होगी।
मजदूर वर्ग में आज ठेकाकरण, अनौपचारिकीकरण, परिधिकरण (पैरीफेरलाइजेशन) तथा नारीकरण (फेमीनाइजेशन) आदि से मजदूरों को संगठित करने की नयी चुनौतियाँ कम्युनिस्टों के सामने हैं। अब लकीर की फकीरी तथा घिसे-पिटे तौर-तरीकों से काम नहीं चलेगा। अब कम्युनिस्टों को मजदूर वर्ग को संगठित करने के नये तौर-तरीके तथा नये सृजनात्मक रूप ईजाद करने होंगे।
मजदूर आन्दोलन में इन चुनौतियों के साथ-साथ नयी सम्भावनाएँ भी पैदा हुई हैं। 1848 में जब ”कम्युनिस्ट घोषणापत्र” में ”दुनिया के मजदूरों एक हो” का नारा दिया गया था, तब वस्तुत: पूरी दुनिया में मजदूर थे ही नहीं, क्योंकि दुनिया के बड़े भाग में पूँजीवादी विकास शुरू न होने के चलते अभी मजदूर वर्ग का जन्म ही नहीं हुआ था। मगर अब पूँजीवाद ने दुनिया के हर मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। आज पूरी दुनिया में मजदूर हैं। आज ‘ग्लोबल असेम्बली लाइन’ पर दुनिया के मजदूरों का हर हिस्सा भौतिक रूप में भी जुड़ चुका है। दूसरे, संचार तथा आवाजाही के साधनों में अभूतपूर्व तरक्की के कारण, दुनिया भर के मजदूरों के आपसी मेलजोल तथा उन्हें विश्वस्तर पर संगठित करने की भी सम्भावनाएँ पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ी हैं।
अपने देश के हालात पर नजर दौड़ाएँ तो आज हमारे देश की आधे से अधिक आबादी शहरी तथा ग्रामीण सर्वहारा, अर्ध्द-सर्वहाराओं की है। करोड़ों की आबादी वाले महानगर अस्तित्व में आ चुके हैं, जहाँ कि गन्दी बस्तियों में करोड़ों-करोड़ उजरती सर्वहारा भरे पड़े हैं। और गौरतलब बात यह है कि आज हमारे देश के औद्योगिक मजदूरों में भारी बहुसंख्या युवा मजदूरों की है। यह युवा मजदूर पुरानी पीढ़ी के मजदूरों से भिन्न है। यह गाँवों से पुरानी पीढ़ी के मजदूरों जितना नहीं जुड़ा है। इस युवा मजदूर का सपना गाँव नहीं है। शहरों में भले लाख मुसीबतें हों लेकिन यह युवा मजदूर गाँव के नीरस, ठहरे, कूपमण्डूकी वातावरण में वापिस नहीं जाना चाहता। दूसरी बात यह है कि यह युवा मजदूर पढ़ा-लिखा है। यह पढ़ा-लिखा युवा मजदूर राजनीतिक रूप से आसानी से शिक्षित हो सकता है और सर्वहारा क्रान्ति की विचारधारा आसानी से आत्मसात कर सकता है। यानी भारतीय सर्वहारा वर्ग (ग्राम्शियन शब्दावली में) अपना ‘ऑर्गेनिक इण्टेलेक्चुअल’ पैदा कर सके, इसके लिए परिस्थितियाँ आज अधिक अनुकूल हैं। यह नया मजदूर भारत के नए मजदूर आन्दोलन का वाहक बनेगा। उम्मीद के उत्स यहीं पर हैं। आज देखा जाए तो मजदूर आन्दोलन के हर पहलू पर निरन्तरता पर परिवर्तन का पहलू हावी है। आज का समय कम्युनिस्ट आन्दोलन के लिए भीषण चुनौतियों तथा बड़ी सम्भावनाओं से भरपूर है। यह समय कम्युनिस्टों से सच्चे वैज्ञानिकों जैसे साहस तथा विवेक की माँग करता है। जरूरत आज इस बात की है कि एक सच्चे वैज्ञानिक के समान आज की देश-दुनिया की बदली हुई परिस्थितियों को स्वीकार किया जाये, उनका अध्ययन-विश्लेषण किया जाये, उन्हें समझा जाये तथा उन्हें बदलने के नये तौर-तरीकों तथा रूपों के बारे में सोचा जाये। और हाँ सिर्फ सोचा ही न जाए, इस सोच-विचार से जो नतीजे निकलें, उन्हें मजदूर आन्दोलन संगठित करने की व्यावहारिक कार्रवाइयों में लागू किया जाये।