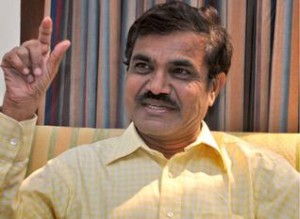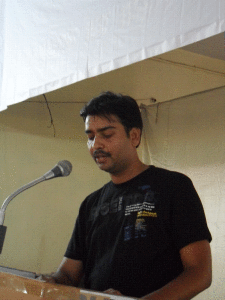बोलिवारियन विकल्पः विभ्रम और यथार्थ
यह 21वीं सदी का नया “समाजवाद” क्या है? इसका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम क्या है? क्या अक्टूबर क्रान्ति के नये संस्करणों का समय सच में ही बीत चुका है? क्या ‘शीत प्रासाद पर धावे’ का युग बीत चुका है? मेस्ज़ारोस के शब्दों में, क्या क्रान्तियों के नये संस्करण अब चुनाव के रास्ते सरकारों में जाने के रूप में ही हो सकते हैं? इस प्रकार के तमाम सवालों का जवाब देकर ही इस ‘21वीं सदी के समाजवाद’ की मूल अन्तर्वस्तु की सही और सटीक पहचान की जा सकती है क्योंकि साम्राज्यवाद-विरोधी होना, कल्याणकारी नीतियों को लागू करना और लोकप्रिय जनवादी संस्थाओं की स्थापना अपने आप में समाजवाद का द्योतक नहीं है। सच है कि अक्टूबर क्रान्ति के नये संस्करण कहीं घटित होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अरब जनउभार, ‘वाल स्ट्रीट कब्ज़ा करो’ आन्दोलन व यूरोप से लेकर एशिया और पूरी दुनिया में उठे छिटपुट आन्दोलन किसी युगान्तरकारी राजनीतिक व आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनों की तरप़फ़ इशारा नहीं कर रहे हैं। आज साम्राज्यवाद के ऐसे दौर में जब पूँजीवाद-विरोधी जनान्दोलन स्वतःस्फूर्त रूप से फूटते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन कहीं भी पूँजीवाद का कोई व्यावहारिक विकल्प खड़ा होता नहीं नज़र आ रहा है, जब अक्टूबर क्रान्ति के नये संस्करण के निकट भविष्य में निर्मित होने की कोई सम्भावना नहीं नज़र आ रही है, तो ऐसे में कोई भी जनपक्षधर स्वप्नद्रष्टा व्यक्ति दो तरह की उम्मीदों में जी सकता है। एक तो है वैज्ञानिक आशावाद जिसमें आशावाद की बुनियाद किसी ठोस समाजवादी मॉडल की वर्तमान दुनिया में मौजूदगी या ऐसे किसी मॉडल के निकट भविष्य में निर्मित हो जाने की सम्भावना नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक इतिहासबोध, जनता और समाज विकास के विज्ञान पर भरोसा होता है। दूसरे किस्म की उम्मीद है एक प्रकार का छद्म आशावाद। इतिहास बोध से वंचित और जनसंघर्षों से कटे तमाम बुद्धिजीवियों को अपने निराशावाद को ढकने के लिए किसी न किसी छद्म विकल्प की ज़रूरत होती है ताकि वे एक छद्म आशावाद में जी सकें। जनता से कटे और हवाई-गुलाबी सपनों में जीने वाले ऐसे बुद्धिजीवी जो कुछ मौज़ूद है उसी से काम चला लेने के पक्षधर होते हैं और पुरानी चीज़ों को ही नये नाम देकर उसे ही नये के…