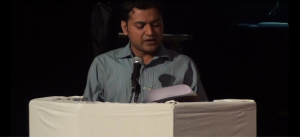पाँचवी अरविन्द स्मृति संगोष्ठी का दूसरा दिन
पेपर में साम्राज्यावादियों, त्रात्सीकीपंथियों और ‘’मुक्त चिंतक मार्क्सवादियों’’ द्वारा स्तालिन के ऊपर लगाये जानेवाले मिथ्या आरोपों का तथ्यों और तर्कों सहित खंडन किया। पेपर में ब्रेस्त-लितोवस्त संधि और गृह-युद्ध के दौरान स्तालिन की भूमिका सम्बन्धित झूठ, ‘’लेनिन की वसीयत’’ के मिथ्या प्रचार, एक देश में समाजवाद स्थापित करने सम्बन्धित विवाद, कृषि में सामूहिकीकरण और कुलक वर्ग के सफ़ाये के दौरान स्तालिन के नेतृत्व में पार्टी द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में दुष्प्रचार, 1936-38 के मुकदमें और शुद्धीकरण की मुहिम के बारे में प्रचारित झूठों, दूसरे विश्व युद्ध के पहले सोवियत-जर्मन समझौते के बारे में इतिहास के विकृतिकरण और वैज्ञानिकों पर दमन सम्बन्धित झूठों का पर्दाफ़ाश किया गया। पेपर में स्तालिनकालीन सोवियत संघ में विज्ञान के प्रोत्साहन से जुड़े कुछ दिलचस्प प्रसंगों का जिक्र किया गया। इसके अतिरिक्त स्तालिन द्वारा पार्टी के भीतर नौकरशाही के खिलाफ़ और जनवाद के लिए किये गये संघर्ष का सप्रमाण ब्योरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ पेपर में स्तालिन के दौर की कुछ गंभीर विचारधारात्मक ग़लतियों को भी रेखांकित किया गया।