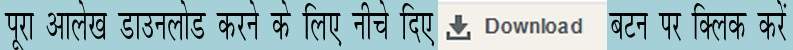नेपाली क्रान्तिः विपर्यय का दौर और भविष्य का रास्ता
आनन्द सिंह
नेपाली क्रान्ति की गाथा बेहद उतार-चढ़ावों से भरी रही है। नेपाली जनता ने कम्युनिस्टों के नेतृत्व में शानदार बहादुराना संघर्ष में अकूत कुर्बानियाँ देकर क्रान्तिकारी आन्दोलन को उस मुकाम तक पहुँचाया जहाँ एक समय वह सारी दुनिया की जनता के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन गया था। लम्बे चले जनयुद्ध के बाद नेपाली क्रान्ति ने राजशाही को इतिहास के कूड़ेदान में धकेलकर एक बड़ी जीत हासिल की। हालाँकि क्रान्ति अभी अधूरी थी लेकिन नेपाल और विश्व की जनता को उससे बहुत उम्मीदें थीं। दूसरी ओर यह भी सच है कि क्रान्ति शुरू से ही अनेक विचारधारात्मक समस्याओं से ग्रस्त थी जो 2008 में संविधान सभा के चुनाव के बाद से बढ़ती गयीं। नेपाल के हालिया घटनाक्रम से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि नेपाली क्रान्ति विच्युति, विचलन, भटकाव और गतिरोध के दौर से आगे निकलकर विपर्यय और विघटन की मंजिल में प्रविष्ट हो चुकी है। 10 नवंबर 2013 को सम्पन्न दूसरी संविधान सभा के चुनावों में एकीकृत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की भारी शिकस्त के बाद इस पार्टी और इसके नेतृत्व की चहुँओर आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि नेपाल और भारत सहित अन्य देशों के तमाम अनुभववादी भावुक क्रान्तिवादी बुद्धिजीवी जो विच्युति और विचलन के दौर में नेपाली क्रान्ति का अनालोचनात्मक महिमामंडन कर रहे थे, वे भी अब निराश और हताश होकर मीन-मेख निकालते हुए नेतृत्व को कोस रहे हैं। दरअसल अनालोचनात्मक महिमामंडन और भयंकर पस्ती और निराशा दोनों का स्रोत एक ही है और वह है मार्क्सवादी विज्ञान की समझ का अभाव और समाज को ऐतिहासिक भौतिकवादी नज़रिये से समझने की बजाय अनुभववादी और भावुकतावादी नज़रिये से देखना। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज जो लोग निराश और हताश होकर कोप भवन में जा चुके हैं वे वही लोग हैं जो कभी अतिउत्साहित होकर माचू पिच्चू के शिखर पर लाल झण्डा फ़हराने के ख़्याली पुलाव पका रहे थे तो कभी सगरमाथा पर लाल झण्डा फहराने को लेकर काफ़ी जोश से भरे थे। इस क़िस्म का अतिउत्साह और निराशा और हताशा दोनों ही मार्क्सवादी विज्ञान की अधकचरी समझ की ही निशानी है। मार्क्सवाद हमें विजय के दौर में भी संयम न खोने और भयंकर से भयंकर पराजय के दौर में भी निराश और हताश होने की बजाय अपनी ग़लतियों का निर्ममता से विश्लेषण कर उन्हें दुरुस्त कर संघर्ष के मोर्चे पर नये संकल्प के साथ जुट जाने की शिक्षा देता है। इसलिए नेपाली क्रान्ति के इस विपर्यय के दौर में भी ज़रूरत इस बात की है कि इसकी कमियों, कमज़ोरियों और विघटन के स्रोतों का निर्ममता से विश्लेषण किया जाये और भविष्य की राह निकाली जाये।
विडंबना यह है कि दूसरी संविधान सभा के चुनावों में एनेकपा (माओवादी) की भारी शिकस्त के बाद भी पार्टी के गम्भीर विचाधारात्मक भटकावों और पहली संविधान सभा के चुनावों के बाद उसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा लिए गये फैसलों की वजह से व्यापक जनता के मोहभंग की स्वीकारोक्ति की बजाय पार्टी इस हार की मुख्य वजह चुनाव के दौरान हुई घपलेबाजी को बता रही है। इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के दौरान घपलेबाजी हुई हो। मतगणना के पहले मतपेटियों को रात भर सेना के बैरक में रखना निश्चित रूप से इस संभावना को बल देता है। परन्तु यदि पार्टी नेतृत्व बुर्जुआ चुनावों को आदर्शवादी नज़रिये से देखकर वाक़ई ‘फ्री एंड फेयर’ सम्पन्न होने के मुग़ालते में था तो इसे उसकी सामाजिक-जनवादी सोच नहीं तो और क्या कहा जायेगा? दूसरी बात यह है कि यदि चुनावी घपलेबाजी के पहलू को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है तो इससे यही संदेश जाता है कि पार्टी इस हार की मुख्य जिम्मेदारी आन्तरिक कमियों और कमज़ोरियों को नहीं बल्कि बाह्य पहलुओं को मानती है। हमारा यह दृढ़ मत है कि यह हार एक लंबे समय से पार्टी में हावी प्रचण्ड और बाबूराम भट्टराई की अवसरवादी संशोधनवादी दक्षिणपंथी लाइन की तार्किक परिणति है।
ग़ौरतलब है कि एक दौर ऐसा भी था जब जनयुद्ध के दौरान प्रचण्ड “वामपंथी” दुस्साहसवादी और सैन्यवादी भटकाव के शिकार थे। विश्व इतिहास में अक्सर ही ऐसा देखने में आया है कि यदि किसी पार्टी में “वामपंथी” भटकाव को राजनीति को कमान में रखते हुए साहसपूर्ण वैज्ञानिक निर्मम आलोचना की बजाय संगठन को कमान में रखकर अवसरवादी तरीके से दूर करने का प्रयास किया जाता है तो अन्ततोगत्वा पेंडुलम “वामपंथी” छोर से दोलन करता हुआ दक्षिणपंथी छोर तक जा पहुँचता है। नेपाल में भी यही हुआ। जनयुद्ध के दौरान नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में बन्दूक को राजनीति के ऊपर रखने की “वामपंथी” सैन्यवादी प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से मौजूद थी। कार्यकर्ताओं की राजनीतिक शिक्षा और समूची पार्टी के बोल्शेविकीकरण पर ज़ोर निहायत ही अपर्याप्त था। ऐसे में यदि दुर्गम जंगलों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों से होता हुआ “प्रचण्ड पथ” जब संसद के आलीशान गलियारों में गुम हो गया तो इसमें क़त्तई आश्चर्य की बात नहीं है। नेपाली क्रान्ति फिसलन भरी ढलान पर तो तभी आगे बढ़ चुकी थी जब तत्कालीन नेकपा (माओवादी) के नेतृत्व के प्रचण्ड धड़े ने सर्वहारा राज्यसत्ता के ‘आर्गन’ के तौर पर सोवियत प्रणाली के बरक्स एक बहुदलीय प्रतिस्पर्द्धात्मक जनवादी प्रणाली के मॉडल को पेश करना प्रारम्भ किया था। समाजवादी संक्रमण, 20वीं सदी के समाजवादी देशों में पूँजीवादी पुनर्स्थापना पर अपनी मौलिक प्रस्थापना देते हुए यह समझ प्रस्तुत की कि समाजवादी देशों में पूँजीवादी पुनर्स्थापना इसलिए हुई क्योंकि वहाँ सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टियों को अन्य पार्टियों से किसी मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टियाँ भ्रष्ट हो गयीं। नेकपा (माओवादी) की यह थीसिस राज्य और क्रान्ति विषयक लेनिन तथा महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति की शिक्षाओं का निषेध थी। यह थीसिस इस पार्टी के संशोधनवाद की ओर प्रस्थान बिन्दु थी।
पहली संविधान सभा के चुनावों के बाद प्रचण्ड के नेतृत्व में नयी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद इस लाइन को और विस्तारित करते हुए ‘प्रतिस्पर्द्धात्मक संघीय गणराज्य’ की स्थापना को तात्कालिक लक्ष्य बनाने की बात की गयी। इस थीसिस के अनुसार पार्टी को फिलहाल संघीय प्रतिस्पर्द्धात्मक संसदीय व्यवस्था के दायरे में ही काम करते हुए सरकार चलानी थी। यानी कि इस लाइन के अनुसार नेकपा (माओवादी) का मुख्य काम सरकार चलाते हुए जनोन्मुख नीतियों के लिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा जनोन्मुख संविधान निर्माण के लिए संघर्ष करना हो गया और एक लंबी प्रक्रिया में बुर्जुआ और संशोधनवादी दलों को चुनावी प्रतिस्पर्द्धा में निर्णायक तौर पर शिकस्त देने के बाद ही लोक जनवादी गणराज्य की दिशा में क़दम बढ़ायेगी। यही नहीं इस घोर संशोधनवादी लाइन की एक और अभिव्यक्ति तत्कालीन नेकपा (माओवादी) के मुखपत्र ‘रेड स्टार’ के सितम्बर 21–30, 2008 के अंक में प्रकाशित पार्टी के विदेश ब्यूरो के सदस्य लक्षमण पंत के एक लेख ‘कोइराला वंश का पतन’ में देखने को आयी जब माक्सर्वादी विज्ञान में “इज़ाफ़ा” करते हुए यह नयी स्थापना दी गयी कि नेपाल में सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग की संयुक्त तानाशाही के रूप में एक नयी राज्यसत्ता अस्तित्व में आ गयी है। यानी सरकार को ही राज्यसत्ता बना दिया गया। मार्क्सवाद का ककहरा भी समझने वाला कोई व्यक्ति यह जानता है कि सरकार राज्यसत्ता नहीं होती। प्रचण्ड के नेतृत्व में मिली-जुली ‘प्राविजनल’ सरकार का गठन सरकार परिवर्तन था, न कि व्यवस्था-परिवर्तन। राज्यसत्ता के प्रमुख अंग सेना, नौकरशाही और न्यायपालिका में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। बुर्जुआ राज्यसत्ता के मुख्य अवलम्ब के रूप में काम करने वाली धार्मिक संस्थाओं की ताकत में कोई कमी नहीं आयी थी, शासक वर्ग के वर्चस्व को दृढ़तापूर्ण स्थापित करने वाली मीडिया पर भी बुर्जुआ ताकतें हावी थीं। जहाँ तक सरकार की बात है तो उसमें भी नेकपा (माओवादी) को सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद स्पष्ट बहुमत न मिलने की वजह से संशोधनवादी और यहाँ तक कि धुर प्रतिक्रियावादी क्षेत्रीय दलों के साथ एक मिली-जुली सरकार बनाना पड़ा था। यानी कि सरकार पर भी इस पार्टी का पूर्ण नियंत्रण नहीं था। ऐसे में लक्ष्मण पंत की स्थापना एक हास्यास्पद बड़बोलापन नहीं तो और क्या थी? ग़ौरतलब है कि ‘रेड स्टार’ में इस लेख के विरोध में कोई टिप्पणी नहीं छपी थी।
हालाँकि प्रचण्ड की लाइन के ख़िलाफ़ नेकपा (एकता केन्द्र – मसाल) ने निरन्तर संघर्ष किया और पार्टी के भीतर भी वैद्य-गजुरेल-बादल धड़े ने तीख़ा संघर्ष किया जिसके कारण इस लाइन को प्रत्यक्षतः पीछे हटना पड़ा, परन्तु जैसा कि बाद के घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया कि यह अवसरवादी लाइन पीछे हटने के बावजूद पार्टी में मौजूद रही। सरकार में बने रहने के दौरान नेकपा (माओवादी) का मुख्य ज़ोर संविधान निर्माण और भूमि-सुधार, रोज़गार के अधिकार, मज़दूरों के अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को मूलभूत नागरिक अधिकार बनाने को लेकर संविधान सभा के भीतर और बाहर संघर्ष करने की बजाय सरकार चलाने पर रहा। बुर्जुआ दलों का भण्डाफोड़ करके अपना आधार विस्तारित करने की बजाय इस पार्टी का मुख्य ज़ोर शासकीय “कल्याणकारी” क़दमों और बुर्जुआ विकास के आधार पर समर्थन बनाना रह गया। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड और तत्कालीन वित्तमन्त्री भट्टराई बुर्जुआ नेताओं की भाँति पूँजीपतियों को भरसक यह आश्वासन देते रहे कि उन्हें पूँजी निवेश का (पढ़िये मज़दूरों को निचोड़ने का) भरपूर मौका मिलेगा। भट्टराई द्वारा प्रस्तुत बजट में भारत और चीन की विकास परियोजनाओं की तर्ज़ पर ‘पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप’ पर बल दिया गया। यह सब इस बेहूदा तर्क की आड़ में किया जा रहा था कि मौजूदा कार्यभार सामन्ती ढाँचे को पूँजीवादी ढाँचे में तब्दील करना था। सरकार में रहते हुए यदि यह पार्टी यथासम्भव जनकल्याणकारी क़दम उठाते हुए भी मुख्य ज़ोर जनता के बीच बुर्जुआ जनवाद की सीमाओं को बेनकाब़ करने पर देती तो यह बात समझी जा सकती थी। परन्तु पार्टी ने इसके ठीक उलट आचरण किया। उसने ऐसे क़दम उठाये जिनको देखकर तमाम देशों की बुर्जुआ जनवादी सरकारों के दिलों में भी नेपाल की ‘प्रॉविज़नल’ सरकार के प्रति सम्मान बढ़ गया होगा। मसलन सरकार ने अध्यादेश जारी करके एक निवेश बोर्ड का गठन किया और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकॉनोमिक ज़ोन) को मंजूरी दी। हद तो तब हो गई जब छह बुनियादी सेवा क्षेत्रों में हड़ताल पर रोक लगाने की क़वायद शुरू हो गई। नेकपा (माओवादी) के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के आचरण से यह दिन के उजाले की तरह साफ़ हो गया कि यह पार्टी बुर्जुआ चुनावों और सरकार के रणकौशलात्मक (टैक्टिकल) इस्तेमाल की बजाय सरकार चलाने को ही अपनी “रणनीति” बना बैठी जिसका ख़ामियाजा उसे देर-सबेर भुगतना ही था।
नेपाली क्रान्ति के अग्रवर्ती विकास के लिए यह आवश्यक था कि सरकार में रहते हुए भी लोकयुद्ध के दौर में मुक्तिक्षेत्रों में जो क्रान्तिकारी लोक सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र बनाये गये थे उनकी हिफ़ाजत करने के साथ ही साथ सतत क्रान्तिकारी प्रचार और उद्वेलन (एजिटेशन) की कार्रवाइयों द्वारा उनको और उन्नत मंजिल पर ले जाया जाता और दोहरी सत्ता जैसी स्थिति बनायी जाती। परन्तु यह माओवादियों का हद दर्ज़े का अदूरदर्शी दक्षिणपंथी अवसरवाद ही कहा जायेगा कि उन्होंने वैकल्पिक लोकसत्ता के केन्द्रों को विकसित करने की बजाय ग्रास रूट स्तर पर जो जनसंस्थायें मौजूद थीं उन्हें भी नष्ट होने दिया। दूसरी संविधान सभा के चुनाव होने तक आलम यह था कि पार्टी अपने पुराने इलाकाई आधारों से उखड़ चुकी थी। यहाँ तक कि लोकयुद्ध के दौरान जो जमीनें भूस्वामियों से छीनकर किसानों में वितरित की गयी थीं उन्हें भी शासक वर्ग के इस आश्वासन के बाद भूस्वामियों को वापस कर दिया गया कि नया संविधान लागू होने के बाद रैडिकल भूमि सुधारों के ज़रिये भूमि का पुनिर्वितरण किया जायेगा। इसी प्रकार शासकवर्ग के सामने निर्लज्जता से घुटने टेकते हुए जनमुक्ति सेना को विलय के नाम पर विसर्जित कर दिया गया। जबकि यदि यह संभव था तो होना तो यह चाहिए था कि शान्ति समझौते के दौरान जनमुक्ति सेना के एक हिस्से को ऊपरी तौर पर विघटित करके जनता के बीच फैला दिया जाता। यदि यह संभव नहीं था तो भी पार्टी को जनता के बीच से आत्मरक्षार्थ स्वयंसेवक दस्ते और जन मिलीशिया के रूप में नये सिरे से जन समुदाय को हथियारबंद करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त हमारा यह भी मानना है कि संविधान सभा में भागीदारी से लेकर सरकार में भागीदारी के पूरे दौर में पूरी पार्टी को खुला करना और क़ानूनी बनाना भी एक भयंकर रणनीतिक चूक थी जो लेनिनवादी पार्टी सिद्धान्त के प्रति अविश्वास का ही परिचायक है। होना तो यह चाहिए था कि प्रोविज़नल सरकार की संक्रमण अवधि का रणकौशल के रूप में इस्तेमाल करते हुए भी पूरी पार्टी को खुला करने की बजाय उसके एक हिस्से को (दूमा धड़े की भाँति) ही खुला किया जाता और उसके भूमिगत ढाँचे को बनाये रखा जाता।
इसके अतिरिक्त प्रोविज़नल सरकार के गठन के दौर में नेकपा (मा.) का मुखपत्र स्वयं पार्टी में मौजूद दक्षिणपंथी अवसरवाद की प्रभावी लाइन की मौजूदगी को साफ़-साफ़ परिलक्षित करता था। ‘रेड स्टार’ में लंबे समय से सांस्कृतिक क्रान्ति, माओवाद, देङ सियाओ पिङ के “बाज़ार समाजवाद” या पूँजीवादी पुनर्स्थापना के बारे में कोई भी विचारधारात्मक सामग्री नहीं दिखाई पड़ी। इस मुखपत्र में प्रमुखता से छपने वाली ख़बरों में चीन की आर्थिक-सामाजिक प्रगति को दर्शाने वाले विवरण, चीनी पार्टी द्वारा नेपाली क्रान्ति और ‘प्रचण्ड की पार्टी’ की प्रशंसा की ख़बरें और क्यूबा की क्रान्ति की प्रगति की ख़बरें रहती थीं। यही नहीं ‘रेड स्टार’ में छपी एक रपट में कोरिया में समाजवाद की प्रगति और ‘जुछे विचारधारा’ की मुक्तकंठ से प्रशंसा की गयी है। यही नहीं बाबूराम भट्टराई ने अपनी अभिव्यक्तियों में प्रचण्ड के संशोधनवाद को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया। उत्पादक शक्तियों के विकास की बात जब वे करते तो ऐसा जान पड़ता मानो देङ सियाओ पिङ की आत्मा उनमें प्रवेश कर गयी है। हद तो तब हो गई जब उन्हें नेपाल जैसे पिछड़े देश में समाजवाद तो दूर लोकजनवादी क्रान्ति की असंभवता को सिद्ध करने के लिए त्रॉत्स्की का भी सहारा लेना पड़ा।
उल्लेखनीय है कि दूसरी संविधान सभा के चुनावों के काफ़ी पहले ही पार्टी के वैद्य-गजुरेल-बादल धड़े ने प्रचण्ड-भट्टराई धड़े को संशोधनवादी बताते हुए उससे खुद को अलग करते हुए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के पुनर्गठन की घोषणा कर दी थी। इस नयी पार्टी ने 33 अन्य पार्टियों के साथ मिलकर दूसरी संविधान सभा के चुनाव का बहिष्कार करने की भी घोषणा की। संविधान सभा के चुनाव में एकीकृत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की बुरी हार की तमाम वजहों में एक वजह यह भी थी। एनेकपा (मा.) के संशोधनवाद का विरोध करते हुए वैद्य-गुजरेल-बादल धड़े ने पुराने जुझारू संगठनकर्ताओं-कार्यकर्ताओं के अच्छे-खासे हिस्से को नेकपा (मा.) का पुनर्गठन करके गोलबंद कर लिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस नयी पार्टी से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह नेपाली क्रान्ति की गाड़ी को पटरी पर ला सकती है?
पुर्नगठित नेकपा (मा.) के नेतृत्व के अतीत के आचरण और इसके मौजूदा दस्तावेज़ों के आधार पर हमें यह उम्मीद बाँधने का कोई कारण नहीं नज़र आता कि यह नयी पार्टी नेपाली क्रान्ति के ऐतिहासिक विपर्यय की स्थिति को बदलकर उसको कोई संवेग देने में सक्षम है। ग़ौरतलब है कि मोहन वैद्य ‘किरण’ ‘प्रचण्ड पथ’ के सबसे मुखर और उत्साही पैरोकारों में से एक थे। उन्होंने ही बड़बोलेपन में आकर इसे ‘इक्कीसवीं सदी की विश्व क्रान्ति की आधारशिला’ तक कह डाला था। पार्टी जब एक ओर धड़ेबन्दी का शिकार थी और दूसरी ओर संसदीय भटकाव के दलदल में धँसती जा रही थी, उस समय बुनियादी विचारधारात्मक सवालों को उठाने की बजाय ‘किरण’ ने सांगठनिक जोड़-तोड़ को ही वरीयता दी। प्रचण्ड जिस समय बहुदलीय संसदीय प्रणाली की बात करते हुए सर्वहारा अधिनायकत्व की अवधारणा को “संशोधित” कर रहे थे, उस समय ‘किरण’ का विरोध मुखर नहीं था। विरोध सर्वाधिक मुखर होकर ‘जनता का जनवाद’ बनाम ‘संघीय जनवाद’ की बहस के दौरान 2008 में सामने आया और उसको भी राजनीति को कमान करने की बजाय संगठन को कमान में रखकर समझौता फॉर्मूले से हल करने की कोशिश की।
प्रचण्ड-भट्टराई-काजीश्रेष्ठ धड़े को नव-संशोधनवादी बताकर अलग होने के बाद किरण-गजुरेल-बादल धडे़ के जो सार्वजनिक दस्तावेज़ उपलब्ध हैं उनमें यह धड़ा बुनियादी राजनीतिक प्रश्नों की बजाय परिधिगत मसलों को ही उठाता दिखाई पड़ता है। समूची पार्टी और पूरे आन्दोलन में व्याप्त गंभीर दक्षिणपंथी विचारधारात्मक भटकावों का निर्मम विश्लेषण करने की बजाय यह व्यक्तिगत दोषारोपण करता हुआ ज़्यादा नज़र आता है। आज इस नयी पार्टी का नेतृत्व भले ही प्रचण्ड को नव-संशोधनवादी बता रहा है, परन्तु उसमें इस बात की आत्मालोचना करने का क्रान्तिकारी साहस नहीं है कि एक वक़्त वे भी इस तथाकथित नव-संशोधनवाद के भागीदार थे।
इसके अतिरिक्त इस नयी पार्टी की आगे की रणनीति और कार्यक्रम संबन्धित जो जानकारियाँ मिल रही हैं उनसे इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि इसमें नेपाली क्रान्ति के ऐतिहासिक विपर्यय की स्थिति को पलटने के लिए आवश्यक विचारधारात्मक क्षमता है। उलटे संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि यह नयी पार्टी भी संशोधनवादी दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पायेगी। हाल ही में विष्णु शर्मा की ऑनलाइन पत्रिका में भारत में सक्रिय इस पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के एक सदस्य के हवाले से बताया गया है कि यह पार्टी अब मानती है कि चूँकि मौजूदा दुनिया बहुध्रुवीय है, अतः इसमें शान्तिपूर्ण संघर्ष की संभावनायें प्रचुर हैं। यदि यह जानकारी सही है तो यह इस नयी पार्टी में संशोधनवाद की एक भयंकर अभिव्यक्ति है। इसके अतिरिक्त यह भी जानकारी मिली है कि यह पार्टी नेपाल को अर्द्ध-सामंती और नव-उपनिवेश मानती है। साथ ही यह संविधान सभा से बाहर रह कर जनांदोलनों के ज़रिये दबाव डालकर ज़्यादा से ज़्यादा जनोन्मुख संविधान बनवाने की पक्षधर है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और जीविका के अन्य मसलों को लेकर जनांदोलन छेड़ने की पक्षधर है। पार्टी यह भी मानती है कि मौजूदा परिस्थितियों में दीर्घकालिक लोकयुद्ध की बजाय जन बग़ावत (पीपल्स इनसरेक्शन) के पहलू पर ज़ोर अधिक देना होगा। ज़ाहिर है कि यह एक अन्तर्विरोधी और असंगत लाइन है क्योंकि यदि नेपाल नव-उपनिवेश है तो वहाँ बुर्जुआ जनवादी स्पेस का कोई सवाल नहीं उठता। ऐसे में जनांदोलन के माध्यम से संविधान बनाने की प्रक्रिया पर दबाव कैसे डाला जा सकेगा? इसके अलावा यदि नेपाल अर्द्ध-सामन्ती और नव-उपनिवेश है तो क्रान्ति के रास्ते में दीर्घकालिक लोकयुद्ध के पहलू को प्रधान होना चाहिए था, परन्तु पार्टी ऐसा नहीं मानती।
उपरोक्त वजहों से यह उम्मीद लगाने का कोई आधार नज़र नहीं आता कि वैद्य-गजुरेल-बादल के नेतृत्व वाली पुनर्गठित नेकपा (मा.) में नेपाली क्रान्ति को संशोधनवाद के दलदल से निकाल पाने की क्षमता है। प्रचण्ड-भट्टराई-काजीश्रेष्ठ के नेतृत्व वाली एनेकपा (मा.) तो पहले से ही इस दलदल में आकंठ डूबी हुई है और उसमें इससे बाहर निकलने की कोई इच्छा भी नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि नेपाली क्रान्ति में संकट का दौर अभी लंबा चलने बाला है। साम्राज्यवादियों का हस्तक्षेप और भारत जैसे प्रभुत्वशाली राष्ट्र की मौजूदगी इस संकट को और जटिल बना देती है। परन्तु यह भी सत्य है कि नेपाली जनता में मुक्ति की आकांक्षायें अभी जीवित हैं और विश्व पूँजीवाद खुद संकट का शिकार है। साथ ही साथ विभिन्न संगठनों में क्रान्ति के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हमें प्रचण्ड और वैद्य की पीढ़ी से तो उम्मीद की कोई किरण नहीं नज़र आती है, परन्तु अगली पीढ़ी से निश्चित ही ऐसे लोग उभरेंगे जो नेतृत्वकारी क्षमता से लैस होकर नेपाली क्रान्ति के इतिहास का निर्ममता से सार-संकलन और विश्लेषण करने का साहस जुटाएंगे। ज़रूरत पिछले 8–10 सालों में संशोधनवादी रोग से ग्रसित पुरानी संरचनाओं के पुनर्गठन की नहीं बल्कि बोल्शेविक साँचे-खाँचे में ढली एक सच्चे अर्थों में लेनिनवादी पार्टी के नये सिरे से पुनर्निमाण की है। आज ज़रूरत मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की युगांतरकारी विचारधारा में “संशोधन” करके इसमें कुछ इज़ाफ़ा करके नया नाम जोड़ने की नहीं बल्कि उसको सच्चे अर्थों में लागू करने की है।