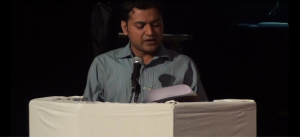भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र: किस हद तक जनवादी
तृतीय अरविन्द स्मृति संगोष्ठी में प्रस्तुत आलेख
– आनन्द सिंह
जब भी कभी नागरिकों के जनवादी अधिकारों की हिफ़ाजत करने में भारतीय लोकतंत्र की विफ़लताओं पर चर्चा होती है तो प्राय: यह तर्क सुनने में आता है कि भारतीय संविधान में कोई कमी नहीं है, कमी तो संविधान को लागू करने वालों में है। इस तर्क के पक्ष में संविधान सभा के समापन भाषण में संविधान के प्रारूप निर्माण समिति के अध्यक्ष डा. भीमराव अंबेडकर का यह कथन प्राय: उद्धृत किया जाता है: “….संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। …” 1
इस प्रकार का तर्क करने वाले लोग भारतीय लोकतंत्र की तमाम विफ़लताओं का ठीकरा संविधान को लागू करने वाली पीढ़ी के सिर पर फोड़ते हैं और संविधान को पाक-साफ़ बताकर उसे प्रश्नेतर बना देते हैं। परन्तु ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि संविधान को लागू करने वाली पीढ़ी दरअसल उसी सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना का उत्पाद होती है जिसको बनाने में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
पूर्व राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन ने भी अपने एक वक्तव्य में कहा था कि संविधान ने हमें नहीं दग़ा दिया है बल्कि हमने संविधान को दग़ा दिया है। श्री नारायणन ने यह बात तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा संविधान की समीक्षा करने हेतु आयोग के गठन के संदर्भ में कही थी। निस्संदेह राजग सरकार का यह कदम निहायत ही गैर-जनवादी तथा भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित था। संविधान के कामकाज की समीक्षा जनमत के आधार पर निर्मित किसी निकाय के बजाय सरकार द्वारा मनोनीत कुछ संविधान विशेषज्ञों एवं चन्द बुद्धिजीवियों द्वारा कराना एक ऐसा गैर-जनवादी कदम था जिसका किसी भी हाल में समर्थन नहीं किया जा सकता। परन्तु संविधान को एक “पवित्र” ग्रन्थ बनाकर प्रश्नों से परे करना भी एक गैर-जनवादी ‘एप्रोच’ है। जनवाद का तकाज़ा तो यह है कि भारतीय लोकतंत्र एवं इसकी विभिन्न संस्थाओं में पिछले छह दशकों के दौरान आये क्षरण की विवेचना के साथ ही साथ इस बात पर भी खुली बहस हो कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया किस हद तक जनवादी थी एवं भारतीय संविधान किस हद तक नागरिकों के अधिकारों की गारण्टी देता है।
कोई भी संविधान जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करे इसके लिये यह बेहद ज़रूरी होता है कि संविधान-निर्माण की प्रक्रिया सार्विक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गयी संविधान सभा द्वारा संपन्न हो। भारत में आज़ादी मिलने के लगभग डेढ़ दशक पहले से ही कांग्रेस पार्टी यह माँग करती रही थी कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु सार्विक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा बुलायी जाये। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ और फ़ैज़पुर के अधिवेशनों में तो जवाहर लाल नेहरू ने इस माँग को केन्द्रीय नारा बनाने की हिमायत की थी। परन्तु भारतीय संविधान को अन्ततोगत्वा जिस संविधान सभा ने निर्मित किया वह सार्विक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की योजना के तहत, परोक्ष रूप से प्रान्तीय असेम्बलियों के उन सदस्यों द्वारा चुनी गयी थी जो स्वयं देश के मात्र 11.5 फ़ीसदी वयस्क नागरिकों द्वारा चुने गये थे। इन प्रान्तीय असेम्बलियों का चुनाव ‘गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट 1935’ के तहत सम्पत्ति एवं शिक्षा जैसे पैमाने द्वारा निर्धारित अतिसीमित निर्वाचक मण्डलों द्वारा किया गया था। यही नहीं, ये निर्वाचक मण्डल धार्मिक एवं जातिगत आधार पर पृथक थे। संविधान सभा में कुल 296 सदस्य थे जिनमें से 96 सदस्य सामंती रियासतों के राजाओं और नवाबों द्वारा मनोनीत किये गये थे। चुने गये सदस्यों में भी अधिकतर संपत्तिशाली एवं अभिजात वर्गों के ही प्रतिनिधि थे। 1946 में कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में पंडित नेहरू ने देश की जनता से यह वायदा किया था कि आज़ादी के बाद संविधान को पारित करने के लिये सार्विक वयस्क मताधिकार पर आधारित एक नयी संविधान सभा बुलायी जायेगी। किन्तु आजा़दी मिलने के बाद इस वायदे को ताक पर रख दिया गया।
संविधान सभा की सभी कार्यवाहियों का मुस्लिम लीग ने संपूर्ण बहिष्कार किया जिसके फ़लस्वरूप संविधान सभा वस्तुत: एकदलीय हो गयी। उसमें जो भी मतभेद उभर कर सामने आये वो कांग्रेस के वामपंथी एवं दक्षिणपंथी धड़ों के बीच के विरोधाभासों की वजह से थे। संविधान-निर्माण के लिए गठित प्रारूप कमेटी ने 27 अक्टूबर 1946 से अपना काम शुरू किया। इण्डियन सिविल सर्विसेज़ के दो नौकरशाहों सर बी. एन. राव एवं एस. एन. मुखर्जी ने संविधान का प्रारूप पहले से ही तैयार कर रखा था। इस सच्चाई को अंबेडकर ने भी प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से 25 नवंबर 1947 में दिये गये भाषण में स्वीकार किया था। प्रारूप कमेटी का काम था पहले से तैयार प्रारूप की जाँच करना एवं आवश्यकता होने पर संशोधन हेतु सुझाव देना। इस तथ्य को संविधान सभा के सदस्य सत्यनारायण सिन्हा ने भी स्वीकार किया था। कमेटी की बैठकें 27 अक्टूबर 1947 से 13 फरवरी 1948 तक जारी रहीं जिनमें प्राय: सभी सदस्य उपस्थित नहीं रहते थे लेकिन कोरम पूरा रहता था। इन बैठकों में कुछ संशोधनों की सिफ़ारिशें की गयीं जिनके आधार पर मूल प्रारूप में चन्द बदलाव किये गये। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के अन्तिम प्रारूप को पारित कर दिया और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया।
संविधान-निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा के बाद आइये देखते हैं कि संविधान की मूल अंतर्वस्तु क्या है। मूल संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 250 तो औपनिवेशिक ‘गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट 1935’ के अनुच्छेदों से हूबहू या फिर थोड़े बहुत शाब्दिक बदलावों के साथ उठा लिये गये थे। ग़ौरतलब है कि यह वही क़ानून था जिसको पंडित नेहरू ने ‘गुलामी के चार्टर’ की संज्ञा दी थी। इस ऐक्ट की धाराओं से बने मूल ढाँचे पर इंग्लैण्ड, अमेरिका, आयरलैण्ड से लेकर कनाडा और आस्ट्रेलिया के संविधानों एवं राजनीतिक परंपराओं से कुछ कुछ प्रावधान उधार लेकर लगभग 90000 शब्दों से सुसज्जित एक वृहदाकार संविधान की रचना की गयी और उसमें लोकलुभावन रंग-रोगन किया गया। प्राय: लोग इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। किन्तु संविधान के आकार और नागरिकों के अधिकारों की हिफ़ाजत करने की उसकी क्षमता का कोई संबन्ध नहीं होता। भारतीय संविधान में तो प्रावधानों का दायरा इतना व्यापक है कि राज्यसत्ता को नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करने के लिये संविधान का उल्लंघन करने की जरूरत ही नहीं है। 1975 का आपातकाल, जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों में वस्तुत: सैन्य तानाशाही जैसी स्थिति, माओवादियों के नाम पर केंद्रीय भारत के आदिवासीबहुल इलाके की जनता के खिलाफ़ युद्ध, तमाम काले कानूनों जैसे घोर गैर-जनवादी कदम आदि सभी पूर्ण रूप से संविधानसम्मत हैं। इस मामले में भारतीय संविधान कुख्यात जर्मन राइख के विधिशास्त्र के क़रीब दिखता है।
संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली में अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना एवं प्रबोधनकालीन आदर्शों की खिचड़ी पकाने की कोशिश दिखती है। मूलभूत अधिकार, न्यायिक समीक्षा, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबन्धी प्रावधान अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। राज्य के नीति निर्धारक सिद्धान्तों की अवधारणा आयरलैण्ड के संविधान से उधार ली गयी है। केन्द्रीकृत संघात्मक ढ़ाँचा कनाडा के संविधान की देन है। समवर्ती सूची की अवधारणा आस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। संसदीय प्रणाली एवं विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच कार्य-विभाजन ब्रिटेन से उधार लिये गये हैं।
भारतीय संविधान की शुरुआत इन शब्दों से होती है:
हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा
उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
अमेरिकी संविधान की शुरुआत भी ठीक ऐसे ही शब्दों से होती है — “हम संयुक्त राज्य के लोग ….”। वैसे देखा जाये तो अमेरिकी संविधान व भारतीय संविधान दोनों की ही शुरुआत धोखाधड़ी से होती है। फिलेडेल्फिया कन्वेंशन, जिसके द्वारा अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें अश्वेत दासों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। भारत की संविधान सभा भी चूँकि सार्विक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गयी थी, वह सच्चे अर्थों में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी।
संविधान लागू होते वक़्त भारत दो शताब्दियों की औपनिवेशिक गुलामी से बदहाल एक अत्यंत पिछड़ा एवं कृषिप्रधान समाज था। ऐसे समाज में क्रांतिकारी ढंग से भूमि सुधार किये बगैर व्यापक आम जनता की सामूहिक पहलकदमी और सामूहिक निर्णय की क्षमता विकसित ही नहीं की जा सकती थी और ऐसा किये बिना साम्राज्यवाद के दबाव व हस्तक्षेप से बचना नामुमकिन था। आज़ादी के बाद अस्तित्व में आयी बुर्जुआ सत्ता तो राजनीतिक रूप से काफ़ी हद तक (पूर्णत: नहीं) सम्प्रभु हुई लेकिन जनता की सम्प्रभुता की दृष्टि से देखा जाय तो प्रस्तावना में ‘सम्प्रभुता सम्पन्न’ शब्द खोखला लगता है। भूमण्डलीकरण के वर्तमान दौर में तो यह शब्द और भी तेजी से अपने मायने खोता जा रहा है।
“समाजवाद” और “धर्मनिरपेक्ष”, ये शब्द मूल संविधान में नहीं थे बल्कि इन्हें 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आपातकाल के दौर में इन शब्दों को प्रस्तावना में ठूँसने का मक़सद दरअसल तत्कालीन इन्दिरा गाँधी सरकार के फ़ासिस्ट और घोर जनविरोधी कृत्यों को लोकलुभावन नारों के आवरण में ढाँकना था और उसका समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के उदात्त आदर्शों से कोई लेना-देना नहीं था। निजीकरण, उदारीकरण और भूमण्डलीकरण के दौर में जब राज्य नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी से भी पल्ला झाड़ रहा है ऐसे में संविधान में “समाजवाद” की मौजूदगी एक त्रासदीय प्रहसन के समान लगती है। रही बात “धर्मनिरपेक्षता” की, तो भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक संस्थाओं, अनुष्ठानों के राज्य और राजनीतिक दायरे से पूर्ण पृथक्करण और धार्मिक विश्वासों को निजी जीवन के दायरे तक सीमित करने के यूरोपीय पुनर्जागरण और प्रबोधन काल से जन्मे क्लासिकीय बुर्जुआ जनवादी अर्थों में नहीं बल्कि “सर्व धर्म समभाव” के रूप में विकसित हुई। ऐसे में यह कतई आश्चर्य की बात नहीं है कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ही धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ता गया है और पूरे देश में सांप्रदायिक, फ़ासीवादी एवं धार्मिेक कट्टरपंथी ताकतें फल-फूल रही हैं।
भारत को विश्व का सबसे बड़ा “लोकतांत्रिक गणराज्य” बताकर इसका गुणगान करने वाले उत्साही समर्थक प्राय: सार्विक वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होने वाले ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष’ चुनावों को इस दावे का आधार बताते हैं। प्रस्तावना में मौजूद आदर्शों में से एक “राजनीतिक न्याय” का भी तात्पर्य इसी आधार से था। इस संदर्भ में यह प्रश्न उठाना लाज़िमी है कि क्या भारी-भरकम पुलिस तंत्र और अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती करके चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करा लेना ही ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष’ चुनावों का पैमाना है? क्या इस समूची प्रक्रिया में बेहिसाब धनबल और बाहुबल का बोलबाला इसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं जनवादी प्रकृति पर प्रश्नचिन्ह नहीं खड़ा करता? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बड़ी पार्टियों ने प्रति उम्मीदवार औसतन 30 करोड़ रुपये खर्च किये एवं छोटी पार्टियों ने औसतन 9 करोड़ रुपये खर्च किये।2 15वीं लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला परन्तु एक ऐसा समूह है जिसको स्पष्ट बहुमत मिला, वह है करोड़पतियों का समूह। 545 सदस्यों वाली लोकसभा में करोड़पतियों की संख्या 300 से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त 150 सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं।3 राज्यों की विधायिकाओं की स्थ्िाति तो इससे भी गई-गुज़री है। ऐसे में स्पष्ट है कि सरकार में आम जनता की नुमाइंदगी क्रमश: कम से कम होती जा रही है। यानि कि इस देश की आम जनता वस्तुत: अपने चुने जाने के अधिकार से वंचित है और उसके चुनने का अधिकार भी सारत: और मुख्यत: औपचारिक ही है। इसके अतिरिक्त चुने गये प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का भी उसे अधिकार नहीं है जिसकी वजह से जनता निरंकुश और गैरजवाबदेह सरकार के सम्मुख अपने आप को लाचार पाती है।
संविधान की प्रस्तावना में घोषित आदर्शों में से एक “आर्थिक न्याय” है। परन्तु संविधान काम करने के अधिकार, न्यूनतम मज़दूरी के अधिकार, काम करने की मानवीय परिस्थितियों के अधिकार, समान काम के लिये समान मज़दूरी के अधिकार, पोषणयुक्त भोजन के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार आदि की कोई गारण्टी नहीं देता। हलाँकि इनमें से कुछ की चलताऊ चर्चा संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों के रूप में की गयी है किन्तु ये सिद्धांत राज्य के लिये विधिक रूप से बाध्यताकारी (justiciable) नहीं हैं। संविधान लागू होते समय यह तर्क दिया गया था कि राज्य के पास अभी इतने संसाधन नहीं हैं कि वह नागरिकों को इन अधिकारों की गारंटी दे सके। संविधान लागू होने के छह दशकों बाद यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि ऐसे समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है; ऐसा क्यों है कि राज्य इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना तो दूर उल्टा इनसे मुकरता जा रहा है। नवउदारवादी नीतियों के दौर में आर्थिक न्याय की बात संविधान के मोटे पोथे में दफ़न निष्प्राण शब्दों के समान लगती है।
सामाजिक न्याय और समता के उद्देश्य को पूरा करने के लिये संविधान में जाति, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिये संविधान के तीसरे भाग में जनता को कुछ मूलभूत अधिकार दिये गये हैं। परन्तु संविधान लागू होने के छह दशक बाद आलम यह है कि भारतीय समाज में जातिगत एवं जेण्डर आधारित संरचनात्मक उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्से में आये दिन घटने वाली दलित उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, कन्याभ्रूणहत्या, बलात्कार, ‘ऑनर किलिंग’ जैसी घटनाएँ संविधान में मौजूद मूलभूत अधिकारों की खिल्ली उड़ाती जान पडती हैं।
जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है, संविधान नागरिकों को इंसानी ज़िन्दगी जीने के लिये ज़रूरी बुनियादी अधिकारों की भी कोई गारण्टी नहीं देता। जिन मूलभूत अधिकारों का जिक्र संविधान के तीसरे भाग में है उनका दायरा बेहद सीमित है। यही नहीं जो अतिसीमित मूलभूत अधिकार संविधान द्वारा प्रदान भी किये गये हैं उन पर भी कानूनी जुमलों का मायाजाल बिछाकर तमाम शर्तों और पाबंदियों के प्रावधान भी संविधान में ही मौजूद हैं जिनका लाभ उठाकर राज्य संविधान की सीमा में रहते हुए भी आसानी से नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है। मिसाल के तौर पर अनुच्छेद 19 को ही लें जिसके तहत नागरिकों को कुछ बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं, जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)(क)), देश में कहीं भी एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)(ख)), संघ बनाने की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)(ग)), भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)(घ)) तथा कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)(ङ))। अनु. 19 में ही यह भी प्रावधान है कि ये सारी स्वतंत्रताएँ ‘उचित प्रतिबंधों’ (reasonable restrictions) के अधीन हैं। इन ‘उचित प्रतिबंधों’ का आधार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता इत्यादि हो सकता है। संविधान में मौजूद इन्हीं ‘उचित प्रतिबंधों’ की आड़ लेकर पिछले छह दशकों में राज्य ने प्रेस की आज़ादी, एकत्र होने और सभाएँ करने से लेकर देश में कहीं भी भ्रमण करने और यूनियन बनाने और हड़ताल करने जैसे बुनियादी जनवादी अधिकारों का धड़ल्ले से हनन किया है। इन ‘उचित प्रतिबंधों’ के अतिरिक्त नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर पाबंदियाँ लगाने के प्रावधान संविधान के अट्ठारहवें भाग में आपातकाल संबन्धी प्रावधानों के रूप में मौजूद हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के घोषित होने की स्थिति में अनु. 20 और 21 में प्रदत्त जीने के एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबन्धी अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूलभूत अधिकार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किये जा सकते हैं। चूँकि ऐसी स्थिति में अनु. 32 में निहित संवैधानिक उपचारों का मूलभूत अधिकार भी निलंबित हो जाता है इसलिये अनु. 20 और 21 में प्रदत्त अधिकार भी वस्तुत: अप्रभावी हो जाते हैं। अब तक देश में तीन बार बाह्य कारणों से और एक बार आन्तरिक कारणों से आपातकाल घोषित किया जा चुका है। जून 1975 से मार्च 1977 तक जा़री आपातकाल नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के व्यापक हनन के लिये कुख्यात है जब संविधान सम्मत तरीके से वस्तुत: तानाशाही कायम थी।
नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का मखौल उड़ाता एक और प्रावधान संविधान के अनु. 22 में मौजूद है जिसके तहत राज्य निवारक निरोध (preventive detention) संबन्धी कानून बनाने के लिये अधिकृत है। इसी संवैधानिक प्रावधान का जमकर लाभ उठाते हुये संसद और राज्य विधायिकाओं ने पिछले छह दशकों के दौरान तमाम काले क़ानून बनाये हैं जिनका इस्तेमाल राज्य ने बड़े पैमाने पर नागरिक अधिकारों के हनन करने के अलावा जनांदोलनों के दमन करने में भी किया। अभी मूल संविधान की स्याही भी नहीं सूखी थी जब संसद ने निरोधक नज़रबंदी क़ानून 1950 (Preventive Detention Act 1950) को पारित किया गया जो 1969 तक प्रभावी रहा। इसके पश्चात 1971 में ‘मीसा’ (Maintenance Of Internal Security Act) लाया गया जो आपातकाल के दौरान राज्य की नग्न तानाशाही का प्रतीक बन गया। 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नामक काला कानून लाया गया जो अभी तक अस्तित्वमान है। 1985 में ‘टाडा’ (Terrorism and Disruptive Activities Act) लाया गया जिसका आतंकवाद से लड़ने के नाम पर जमकर दुरुपयोग हुआ। 2002 में तत्कालीन राजग सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिये अभूतपूर्व तरीके से पहले अध्यादेश जारी करके और फिर संसद की संयुक्त बैठक बुलाकर ‘पोटा’ (Prevention of Terrorism Act) को पारित करवाया जिसका दुरुपयोग होना ही था और वही हुआ। 2004 में संप्रग सरकार ने अपनी प्रगतिशील छवि दिखाने के लिये पोटा को निरस्त किया लेकिन बड़ी ही चतुराई से उसके काले प्रावधान गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) कानून (Unlawful Activities (Prevention) Act) में डाल दिये। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में इस किस्म के काले क़ानून अभी तक विद्यमान हैं, मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में ‘मकोका’ और छत्तीसगढ़ में ‘छत्तीसगढ़ विशेष सुरक्षा अधिनियम’।
अभी हाल ही में पी.यू.सी.एल. द्वारा दिल्ली में आयोजित राज्य के दमन-विषयक संगोष्ठी में देश भर से आये नागरिक आजा़दी एवं जनवादी अधिकार कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव साझा किये कि किस प्रकार देश के अलग-अलग हिस्सों में राज्य मशीनरी काले कानूनों को जनांदोलनों के दमन के लिये एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल कर रही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में काले कानूनों का इस्तेमाल मज़दूर व किसान नेताओं एवं जनांदोलनों से सहानुभूति रखने वाले मीडियाकर्मियों तथा बुद्धिजीवियों के खि़लाफ़ किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में राजद्रोह कानून (भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क) का विशेष उल्लेख किया गया जिसके तहत बिनायक सेन जैसे तमाम बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं के खि़लाफ़ मुकदमे चलाये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह धारा औपनिवेशिक दौर से ही चली आ रही है जिसके तहत तिलक और गाँधी पर भी मुकदमे चलाये गये थे।
इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों एवं जम्मू–कश्मीर में वस्तुत: सैनिक शासन को मान्यता भी ‘सैन्य बल विशेष अधिकार अधिनियम’ जैसे काले कानून द्वारा मिली हुई है। पूर्वोत्तर में यह काला कानून 1958 से तथा जम्मू–कश्मीर में 1990 से लागू है जिसकी आड़ में सैन्य बलों ने परिधि की इन राष्ट्रीयताओं की जनता के नागरिक एवं जनवादी अधिकारों का खूब हनन किया है। गौरतलब है कि इन क्षेत्रों में वस्तुत: सैनिक शासन जैसी स्थिति बिल्कुल संविधानसम्मत है। जम्मू–कश्मीर के मामले में तो भारतीय राज्य ने जनमत-संग्रह कराने के अपने वायदे से मुकरकर बड़ी ही चतुरार्इ से अनु. 370 के संवैधानिक अस्त्र द्वारा वहाँ की जनता की मर्ज़ी के बगैर उसका क्रमश: भारत में विलय कर लिया।
भारत के औपनिवेशिक अतीत की काली छाया संविधान और काले कानूनों में ही नहीं बल्कि शासन-प्रशासन के समूचे ढाँचे पर स्पष्ट दिखायी पड़ती है। पिछले वर्ष एक संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाषण देते वक्त पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने रैडिकल तेवर दिखाते हुए पारंपरिक गाउन को उपनिवेशवाद का बर्बर अवशेष चिन्ह बताते हुए उतार फेंका। परन्तु मंत्री महोदय शायद यह भूल गये कि महज़ गाउन ही नहीं बल्कि केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रालय और सचिवालय से लेकर जिला और तहसील के स्तर तक शासन-प्रशासन के ढाँचे, कार्यप्रणाली एवं मानसिकता में भी उपनिवेशवाद के बर्बर अवशेष चिन्ह आज भी मौजूद हैं। भारतीय शासन-प्रशासन को संचालित करने वाले लगभग सभी मुख्य कानून उपनिवेशवाद के दौर में औपनिवेशिक शासन को संचालित करने के लिए बनाये गये थे जिनको आज़ादी मिलने के बाद जस का तस या चन्द बदलावों के साथ अपना लिया गया। मिसाल के तौर पर भारतीय दंड संहिता 1860 में बनायी गयी थी, इण्डियन एविडेंस एक्ट 1872 में बनाया गया था, सिविल प्रोसीज़र कोड 1908 में बनाया गया था, ट्रांसफ़र ऑफ प्रापर्टी एक्ट 1882 में बनाया गया था। इसके अतिरिक्त अतिकेन्द्रीकृत, अपारदर्शी, पदसोपानक्रम आधारित प्रशासनिक ढाँचा, कार्यप्रणाली, नौकरशाहों के ओहदे, उनका जनता से कटाव — ये सभी औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाते हैं। दो शीर्षस्थ ऑल इण्डिया सर्विसेज IAS और IPS (जिनका जि़क्र संविधान में भी है) भी उपनिवेशवाद की देन है। IAS की पूर्ववर्ती ICS ब्रिटिश राज की ‘स्टील फ्रेम’ मानी जाती थी जिसके दम पर समूचा औपनिवेशिक प्रशासन टिका हुआ था। आज़ादी के बाद भी IAS की भूमिका शासक वर्गों के निरंकुश शासन की निरंतरता को बनाये रखने में ही ज़्यादा प्रभावी रही है। जहाँ तक जनकल्याण एवं विकास संबन्धी ज़िम्मेदारियों का प्रश्न है, उनमें यह घोर जनविरोधी और फिसड्डी साबित हुई है। उपनिवेशवाद की छाप नौकरशाहों की मानसिकता और जनता के साथ उनके बर्ताव में भी साफ़ झलकती है। सिविल सर्विसेज की दशा का निरीक्षण करने हेतु 2001 में गठित वाई. के. अलग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सही ही कहा था कि सिविल सर्विसेज के सदस्य “शासक मानसिकता” से ग्रसित होते हैं।
भारत मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (The Universal Declaration of Human Rights) और मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (International Covenant of Human Rights) का हस्ताक्षकरकर्ता है। परन्तु यह एक विडंबना है कि इसके बावजूद भारत में राज्य के विभिन्न अंगों द्वारा मानवाधिकारों का हनन एक आम बात है। भारतीय पुलिस बल गैर कानूनी हिरासत, हिरासत में मौतों एवं बलात्कार, फ़र्जी मुठभेड़ों आदि के लिए कुख्यात है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए. एन. मुल्ला ने एक फै़सले में टिप्पणी करते हुए कहा था, “पूरे देश में ऐसा एक भी अराजक ग्रुप नहीं है जिसके द्वारा किये गये अपराध भारतीय पुलिस नामक संगठित गिरोह द्वारा किये गये अपराधों के तुल्य हो।” एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2001 और 2009 के बीच भारतीय पुलिस हिरासतों में 1,184 लोग मारे गये।4 एक आर.टी.आई. कार्यकर्ता की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में होने वाली हर दूसरी पुलिस मुठभेड़ फ़र्जी होती है।5 मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिये बनाया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नितांत अप्रभावी साबित हुआ है।
भारतीय जनमानस में विधायिका और कार्यपालिका की छवि तो बहुत पहले ही धूमिल हो चुकी थी, किन्तु कुछ दशकों पहले तक न्यायपालिका की छवि अपेक्षाकृत बेहतर थी। न्यायपालिका को नागरिकों के जनवादी अधिकारों की दृष्टि से उम्मीद की आखि़री किरण समझा जाता था। परन्तु वक़्त गुज़रने के साथ ही साथ उम्मीद की यह आख़िरी किरण भी मद्धिम होती जा रही है। न्याय की प्रक्रिया दिन-प्रतिदिन अधिक खर्चीली, लंबी और थकान भरी होती जा रही है। संवैधानिक उपचार (constitutional remedies) तो पहले ही आम जनता की पहुँच से बाहर थे, जिन कानूनी उपचारों (legal remedies) की पहुँच उन तक है भी, उनकी प्रक्रिया भी इतनी जटिल और थकाऊ है कि इस प्रक्रिया से गुज़रना अपने आप में एक सज़ा से कम नहीं है। देश के विभिन्न न्यायालयों में 3 करोड़ से भी अधिक मुकदमे लंबित हैं। एक आकलन के मुताबिक यदि भारतीय न्यायालय मौजूदा रफ़्तार से न्याय देते रहेंगे तो इन लंबित मामलों को निपटाने में कुल 320 वर्षों से भी अधिक का समय लग जायेगा।6 भारतीय जेलों में लगभग 70 फ़ीसदी कैदी अण्डरट्रायल हैं जो अपने आप में राज्यसत्ता द्वारा नागरिकों के मानवाधिकारों के हनन की एक जिन्दा मिसाल है। भारतीय न्याय व्यवस्था श्रम कानूनों को लागू करवाने एवं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करवाने में भी नितांत विफ़ल रही है। श्रम न्यायालयों और औद्योगिक ट्राइब्युनलों से न्याय मिलने में इतना विलम्ब होता है कि ज़्यादातर गरीब और मज़दूर वहाँ जाने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। उदारीकरण और भूमण्डलीकरण के इस दौर में उच्च न्यायपालिका ने अमूमन श्रम-विरोधी रुख़ ही अपनाया है।
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ (Centre For Media Studies) द्वारा कराये गये एक देशव्यापी सर्वे के मुताबिक सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले लोगों में से 77 फ़ीसदी लोगों की राय में भारतीय न्याय व्यवस्था भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार का दायरा अब निचली अदालतों तक ही नहीं रहा। वर्ष 2002 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश एस. पी. भरूचा ने कहा था कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों में 20 फ़ीसदी भ्रष्ट हैं। तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब तो सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश तक भ्रष्टाचार की चपेट में आ गये हैं। ऐसे में न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के जनवादी अधिकारों की हिफ़ाजत करने की क्षमता पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लग जाता है।
ऐसा नहीं है कि भारतीय शासन एवं प्रशासन व्यवस्था को औपनिवेशिक अतीत के बोझ से मुक्त कराकर ज़्यादा जनोन्मुखी बनाने के बारे में कभी सोचा नहीं गया। अब तक देश में संविधान के कामकाज की समीक्षा आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, पुलिस आयोग, विधि आयोग और प्रशासनिक सुधार संबन्धी अनगिनत कमेटियाँ बन चुकी हैं। यह बात दीगर है कि इन आयोगों और कमेटियों की ढेरों सिफ़ारिशें उपनिवेशकाल के समय से ही चली आ रही फाइलों के नीचे धूल फाँक रही है। औपनिवेशिक अतीत का यह बोझ इतना भारी हो गया है कि इससे मुक्ति पाना आयोगों और कमेटियों के बस की बात नहीं है और न ही शासक वर्ग में ऐसी कोर्इ इच्छाशक्ति मौजूद है। अपने जनवादी अधिकारों की रक्षा करने के लिये जनता के सम्मुख अब बस जनांदोलनों का ही रास्ता बचा है। जनवादी अधिकार आंदोलन को यह सच्चाई आत्मसात करनी ही होगी और इसके अनुसार अपना एजेण्डा सेट करना होगा।
जनवादी अधिकार कार्यकर्ताओं को जनांदोलनों के माध्यम से जनता को जनवादी अधिकारों के अर्थ एवं उनके महत्व के बारे में देश की व्यापक आम आबादी को शिक्षित करना होगा। उनको जनवादी अधिकारों के मुद्दों पर एकजुट, लामबंद तथा संगठित करना होगा। सभी औपनिवेशिक तथा काले कानूनों एवं पुलिस-प्रशासन की सभी जनविरोधी कार्रवाइयों के खि़लाफ़ देशव्यापी स्तर पर जनांदोलन चलाने होंगे। गौरतलब है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दोरान भी देश स्तर पर जनांदोलनों की शुरुआात रॉलेट ऐक्ट जैसे काले कानून — जो दरअसल वर्तमान काले कानूनों का वास्तविक अर्थों में पूर्वज है, के ख़िलाफ जनता की व्यापक लामबंदी से हुई थी। जनांदोलनों के दौरान ही मौजूदा केन्द्रीकृत, अपारदर्शी एवं जनविरोधी संस्थाओं के विकल्प भी तलाशने होंगे। बड़े निर्वाचक मंडलों की बजाय छोटे-छोटे निर्वाचक मंडलों के आधार पर बहुसंस्तरीय चुनाव प्रणाली एवं निर्वाचित सदस्यों को वापस बुलाने के अधिकार के बारे में भी गम्भीरता से सोचना होगा। नौकरशाही पर नकेल कसने के लिए प्रशासन के विभिन्न संस्तरों पर जनता द्वारा चुनी गई जन समितियों और जन-परिषदों के नानाविध रूप विकसित करके शासन-प्रशासन की कार्यवाही में आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी एवं सहभागिता बढ़ाने की दिशा में भी संजीदगी से विचार करना होगा। ज़ाहिर है कि इतने बड़े पैमाने पर संवैधानिक, कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था में फ़ेरबदल के लिये जनाधार तैयार करने के लिये जनवादी अधिकार आंदोलन को सार्विक वयस्क मताधिकार पर आधारित एक नयी संविधान सभा बुलाये जाने की माँग को भी अपने एजेण्डे पर रखना होगा।
References
1. Ambedkar’s speech before the constituent assembly on 25 November 1947
2. Amit Bhaduri’s article in EPW, November 2010
3. National Election Watch (http://nationalelectionwatch.org)
4. Report of Asian Centre of Human Rights (http://www.achrweb.org/countries/india.htm)
5. Two Circles (http://www.achrweb.org/countries/india.htm)
6. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-03-06/india/28143242_1_high-court-judges-literacy-rate-backlog